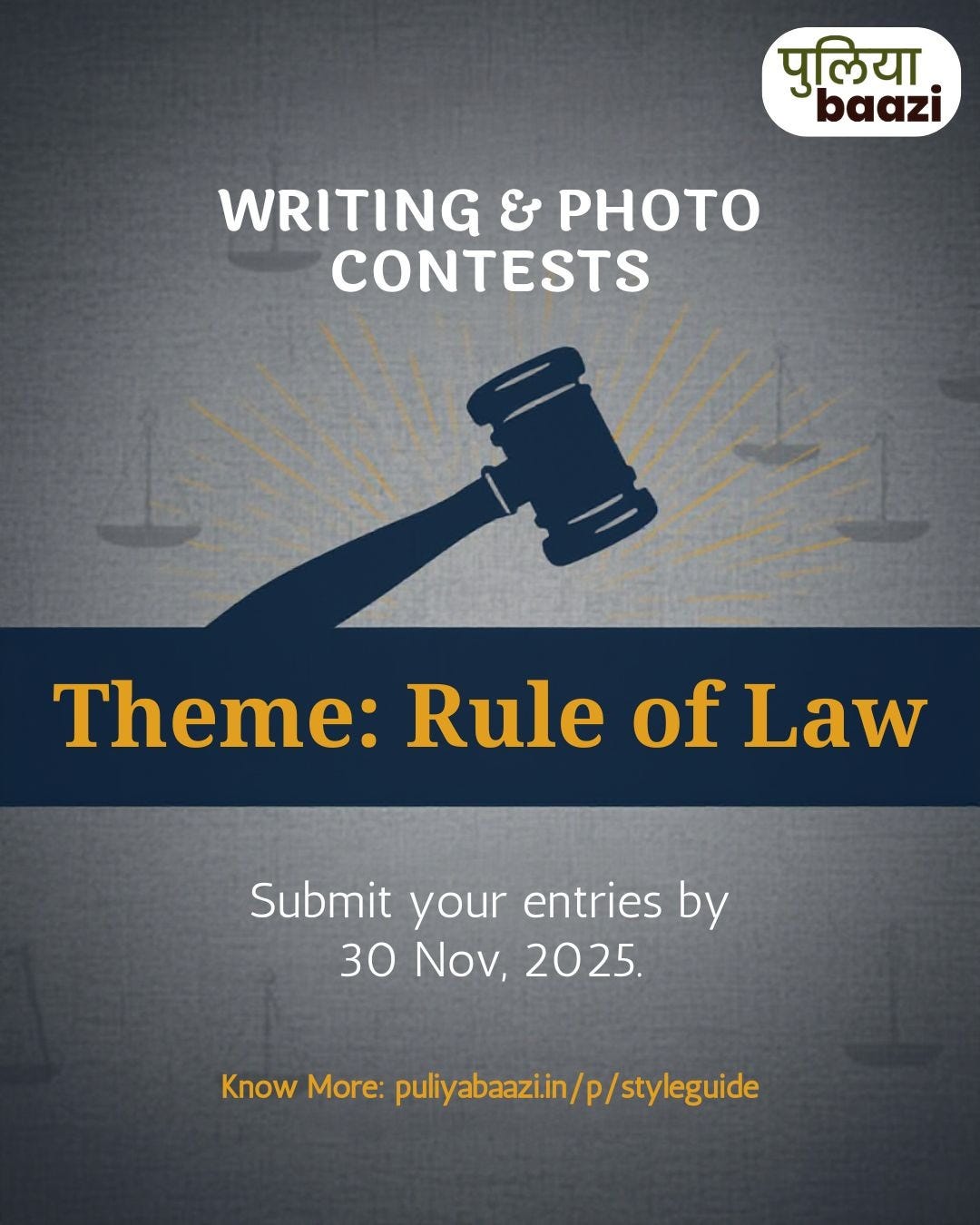भारत की विकास यात्रा : कबीरदास की उलटबाँसी | India's Premature Leapfrogging
Seven Insights from ‘A Sixth of Humanity’
A Sixth of Humanity: Independent India’s Development Odyssey यह एक ऐसी किताब है, जिसे भारत की पब्लिक पॉलिसी में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान को पढ़ना चाहिए। जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट देवेश कपूर और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने इस किताब में अपने जीवनभर के अध्ययन का निचोड़ पेश किया है।
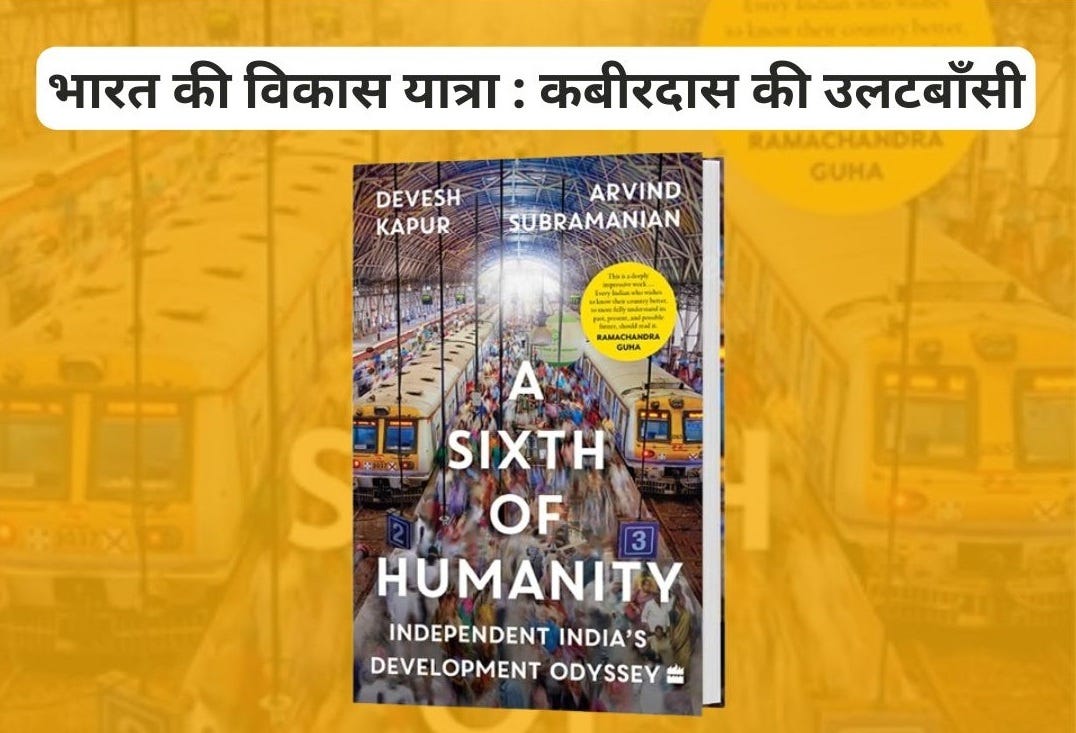
इसमें कई चार्ट, टेबल और आँकड़े दिए गए हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। साथ-ही इसमें 150 पन्नों के नोट्स भी हैं, जिससे किताब की गहराई समझ में आती है। इस किताब को धीरे-धीरे, समझते हुए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपको एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आइए, देखते हैं ऐसे ही कुछ मुद्दे:
1991 से 2020 के बीच, भारत का औसत फिस्कल डेफिसिट सभी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे ज़्यादा था। इन अर्थव्यवस्थाओं में तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना और चीन भी शामिल हैं। [हालाँकि भारत ने इस दौरान अपना कर्ज़ कभी नहीं डुबाया, लेकिन यह तगड़ा घाटा हमारे भविष्य पर लगातार असर कर रहा है।]
हर साल औसतन 50% से ज़्यादा भारतीय वोट डालने जाते हैं क्योंकि देश में कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। [लेकिन इस किताब के लेखक ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ का समर्थन नहीं करते, वे दूसरे रास्ते सुझाते हैं।]
केरल की GSDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा, सऊदी अरब की GDP में मैन्युफैक्चरिंग के हिस्से से भी कम है। सऊदी अरब के पास तेल और गैस के भंडार हैं और इसलिए उसकी GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नाममात्र है, लेकिन केरल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का न होना बहुत बड़ी असफलता है। [सोचिए, हमने कितना बड़ा मौका गँवा दिया!]
विदेशों में बसे चीनी नागरिकों से चीन में आया हुआ FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशों में बसे भारतीयों से भारत में आए FDI से 20-25 गुना ज़्यादा था। [FDI ने चीन की तरक्की में गज़ब की तेज़ी लाई, जबकि भारत की नीतियों ने इस रास्ते पर ब्रेक लगा दिया।]
चीन में ‘इंटरनल माइग्रेशन’ की दर भारत से ज़्यादा है। [...वो भी तब जब वहाँ Hukou जैसी सख्त पाबंदियाँ हैं, जो लोगों को आसानी से शहर बदलने नहीं देतीं।]
मंडल कमीशन ने किसी जाति को ‘सामाजिक रूप से पिछड़ा’ मानने के लिए जो ग्यारह शर्तें लगाई थीं, उनमें से एक यह थी कि—‘क्या उस जाति में काम करने वाली महिलाओं का हिस्सा, राज्य के औसत से 25% ज़्यादा है?’। इसका मतलब यह हुआ कि कमीशन की नज़र में, कम महिलाओं का काम पर जाना तरक्की की निशानी थी, पिछड़ेपन की नहीं! [यह तो सब जानते हैं कि भारत में जब परिवार की आमदनी कम होती है, तभी घर की महिलाएँ काम करने जाती हैं। लेकिन पिछड़ेपन के लिए इस शर्त का इस्तेमाल करके, सरकार ने एक तरह से महिलाओं को लेकर हमारी दकियानूसी सोच पर ही मुहर लगा दी।]
2019 और 2023 के बीच, सरकार ने अकेले BSNL में 3 ट्रिलियन (3 लाख करोड़) रुपये से ज़्यादा झोंक दिए। [शायद इसमें से कुछ पैसा स्वदेशी 4G तकनीक बनाने में गया हो, जिसकी घोषणा आखिरकार सितंबर 2025 में की गई!]
इस किताब का हर चैप्टर ज्ञान और जानकारी से ओतप्रोत भरा हुआ है। लेकिन, जिस हिस्से ने मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया, वह था चीन और भारत के कृषि क्षेत्र की तुलना। लेखकों का कहना है कि भारत के विकास में सबसे बड़ी गड़बड़ी प्लानिंग करने, बड़े सरकारी कारखाने लगाने या एक्सपोर्ट को नज़रअंदाज़ करने से नहीं हुई। इनमें से हर एक बात उस वक्त के कई बड़े अर्थशास्त्री सुझा रहे थे। आज़ादी के बाद पहले तीन दशकों में भारत में बुनियादी बदलाव न होने की असली वजह थी—कृषि क्षेत्र पर ध्यान न देना और भारत के अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करना।
जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और 1978 के बाद वाले चीन ने यह समझा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए पहले खेती की पैदावार बढ़ाना ज़रूरी है। वहीं दूसरी ओर, भारत, सोवियत संघ और 1978-पूर्व चीन ने खेती को इंडस्ट्रियलाइजेशन से ध्यान भटकाने वाली चीज़ माना।
इस दूसरी सोच के मुताबिक, खेती का काम बस इंडस्ट्री के लिए सस्ता अनाज और सस्ते मज़दूर मुहैया कराना था। उन्हें डर था कि अगर खेती में पैदावार बढ़ गई, तो मज़दूरी बढ़ जाएगी और इससे इंडस्ट्री का बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इस सोच के चलते, कृषि सुधार, नई तकनीक आदि में सरकारी निवेश, गाँवों में कर्ज़ वितरण और भूमि सुधार कानून जैसे ज़रूरी काम ठंडे बस्ते में पड़ गए। नतीजा? भारत में खेती की पैदावार गिरती चली गई।
इसी वजह से 1960 और 1970 के दशक में देश में भयंकर खाद्य संकट आ गया और भारत की कुल आयात में सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों का हिस्सा लगभग 20% तक बढ़ गया। इस गलती को 1970 के दशक में हरित क्रांति के ज़रिये सुधारा गया। खूब सब्सिडी दी गई और कुछ खास फ़सलों पर MSP भी दिया गया। इससे अनाज का संकट तो टल गया, लेकिन आगे चलकर कई दूसरी, गहरी समस्याएँ खड़ी हो गईं। इसके उलट, चीन में माओ के ज़माने की भारी उथल-पुथल के बावजूद, खेती की पैदावार लगातार बढ़ती रही।
भारत की विकास यात्रा का दूसरा सबसे अलग पहलू यह था कि उसने लाइसेंस-राज और राष्ट्रीयकरण के ज़रिये अपने ही देश के प्राइवेट सेक्टर का गला घोंट दिया। उस ज़माने में दुनिया के कई विकासशील देशों ने इम्पोर्ट सब्स्टीट्यूशन यानी आयात के बजाय घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति अपनाई थी, लेकिन किसी भी देश ने अपनी प्राइवेट कंपनियों के साथ वैसा नफ़रत भरा बर्ताव नहीं किया था, जैसा भारत ने किया। यह लाइसेंस-राज हमारी सिस्टम में इतना गहरा उतर चूका था कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को इसे एकदम सावधानी से, चोरी-छुपके खत्म करना पड़ा। यहाँ तक कि तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 1991 के मशहूर बजट भाषण में भी इसका ज़िक्र नहीं किया गया।
किताब के इस हिस्से को पढ़ने के बाद, भारत की शुरुआती कृषि नीतियों के बारे में मेरी सोच काफ़ी हद तक बदल गई। क्या आपकी भी?
इस किताब के बारे में और जानने के लिए, इसके लेखकों के साथ हुई पुलियाबाज़ी ज़रूर सुनें।
—प्रणय कोटास्थाने
अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी
यही लेख आप अंग्रेज़ी में यहाँ पढ़ सकते हैं: Making Sense of India’s Developmental Choices
प्रणय कोटास्थाने के अन्य लेख और चर्चाएँ आप पुलियाबाज़ी और Anticipating the Unintended पर पढ़ सकते हैं।
We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.
Puliybaazi Photo & Writing Contest
प्रिय पाठक,
पुलियाबाज़ी की कोशिश हमेशा से यही रही है कि यह संवाद दोतरफा हो। इसलिए हम समय-समय पर आपको पुलियाबाज़ी से जुड़ने का आह्वान करते आए हैं, फिर चाहे वो हमारा 300वां एपिसोड ‘आपके सवाल, हमारे जवाब’ हो या फ़ोटो कॉन्टेस्ट और राइटिंग कॉन्टेस्ट जैसी प्रतियोगिताएँ। हमारे इन प्रयासों को जब आपकी तरफ़ से सकारात्मक प्रतिसाद मिलता है, तब हमारा उत्साह और बढ़ता है और आपके लिए नए विषय तथा नए मेहमान लाने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इन प्रतियोगिताओं में ज़रूर शामिल हुआ करें, इससे आप भी पुलियाबाज़ी का सही मायने में लुफ़्त उठा पाएँगे।
पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के दूसरे अंक का काम शुरू हो गया है। इस बार हम आपके लिए ‘रुल ऑफ़ लॉ’ की थीम पर एक से बढ़कर एक लेख लेकर आ रहे हैं। पिछली बार की तरह हम चाहते हैं कि इस बार भी आप इस मैगज़ीन का हिस्सा बनें। इसलिए हमने फ़ोटो कॉन्टेस्ट और राइटिंग कॉन्टेस्ट की घोषणा की है। तो देर किस बात की, ‘रुल ऑफ़ लॉ’ की थीम पर भेजिए अपने फ़ोटो और लेख जल्द से जल्द।
अधिक जानकारी यहाँ देखिए: https://www.puliyabaazi.in/p/styleguide