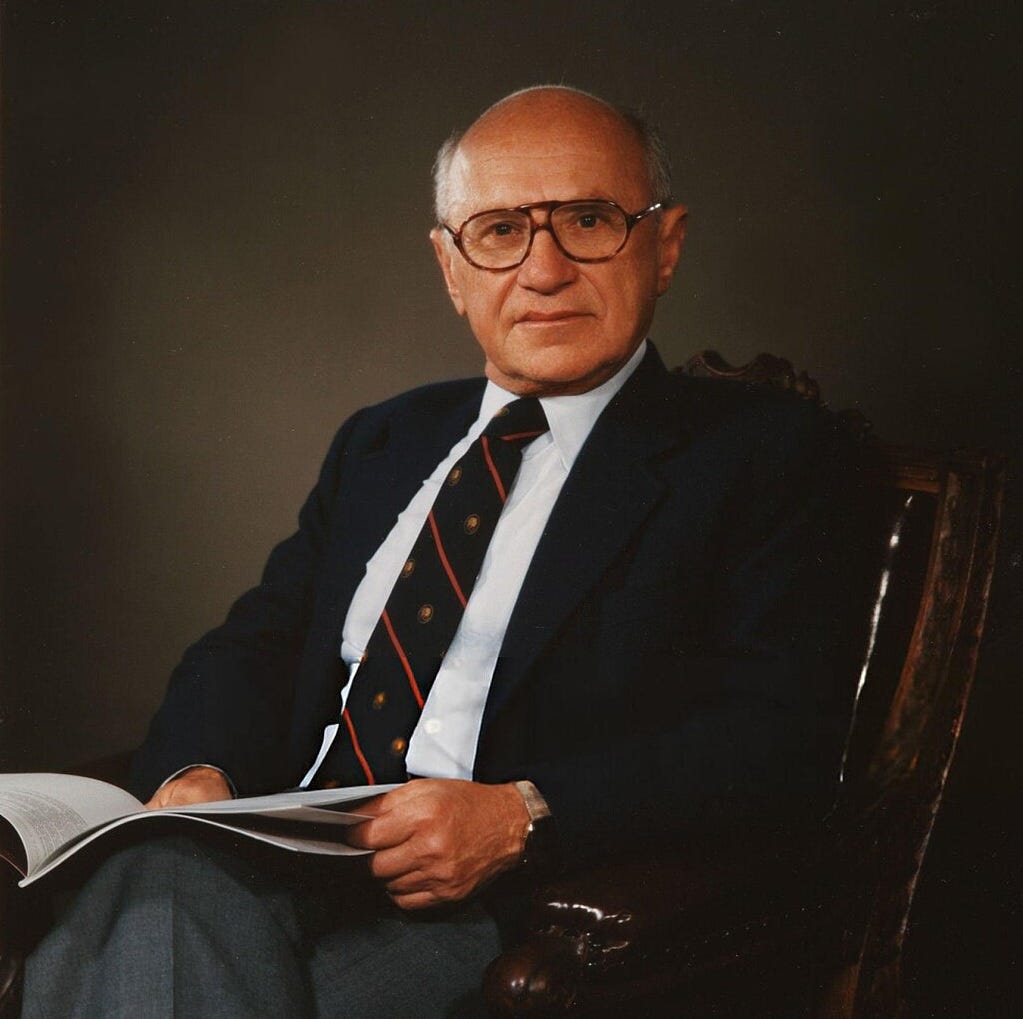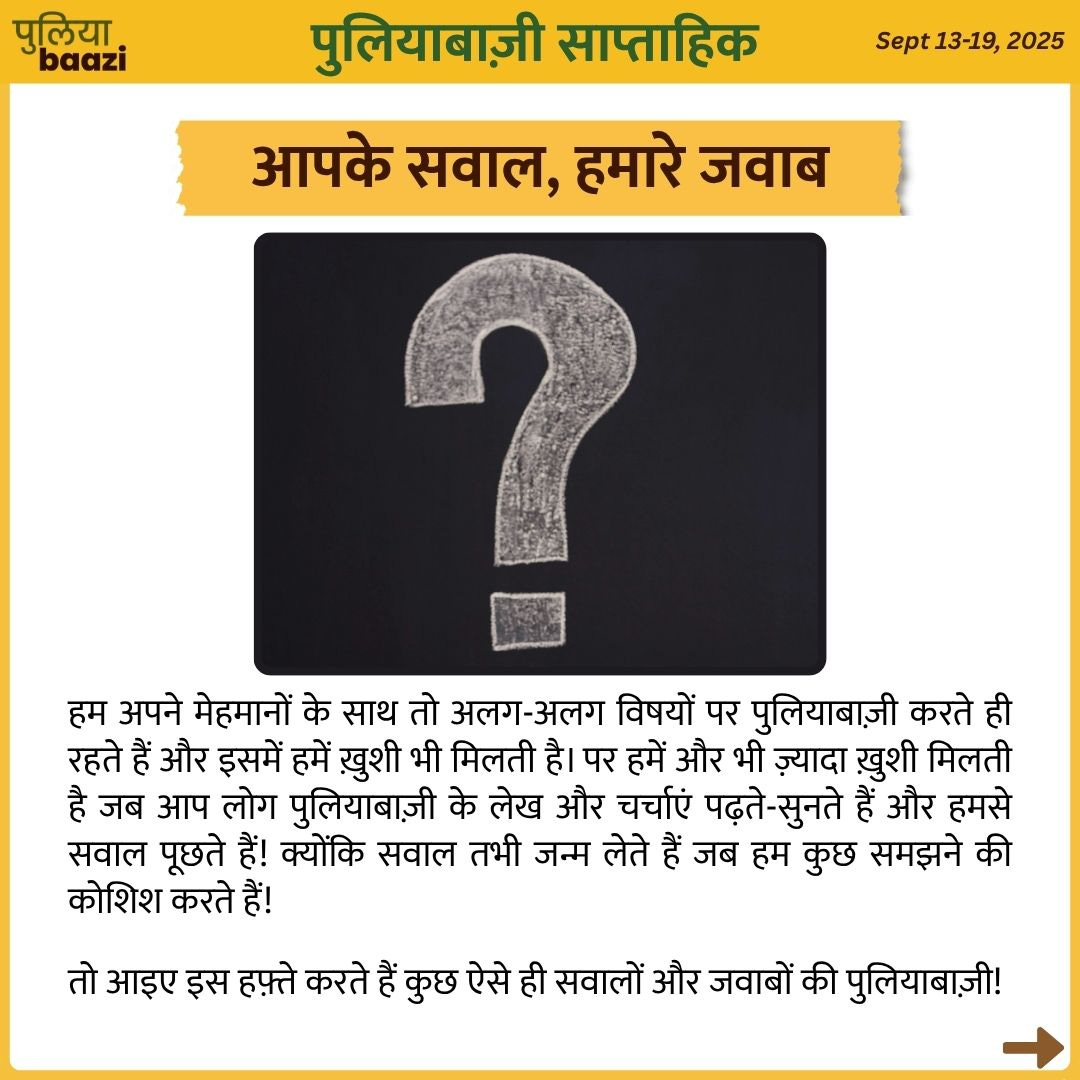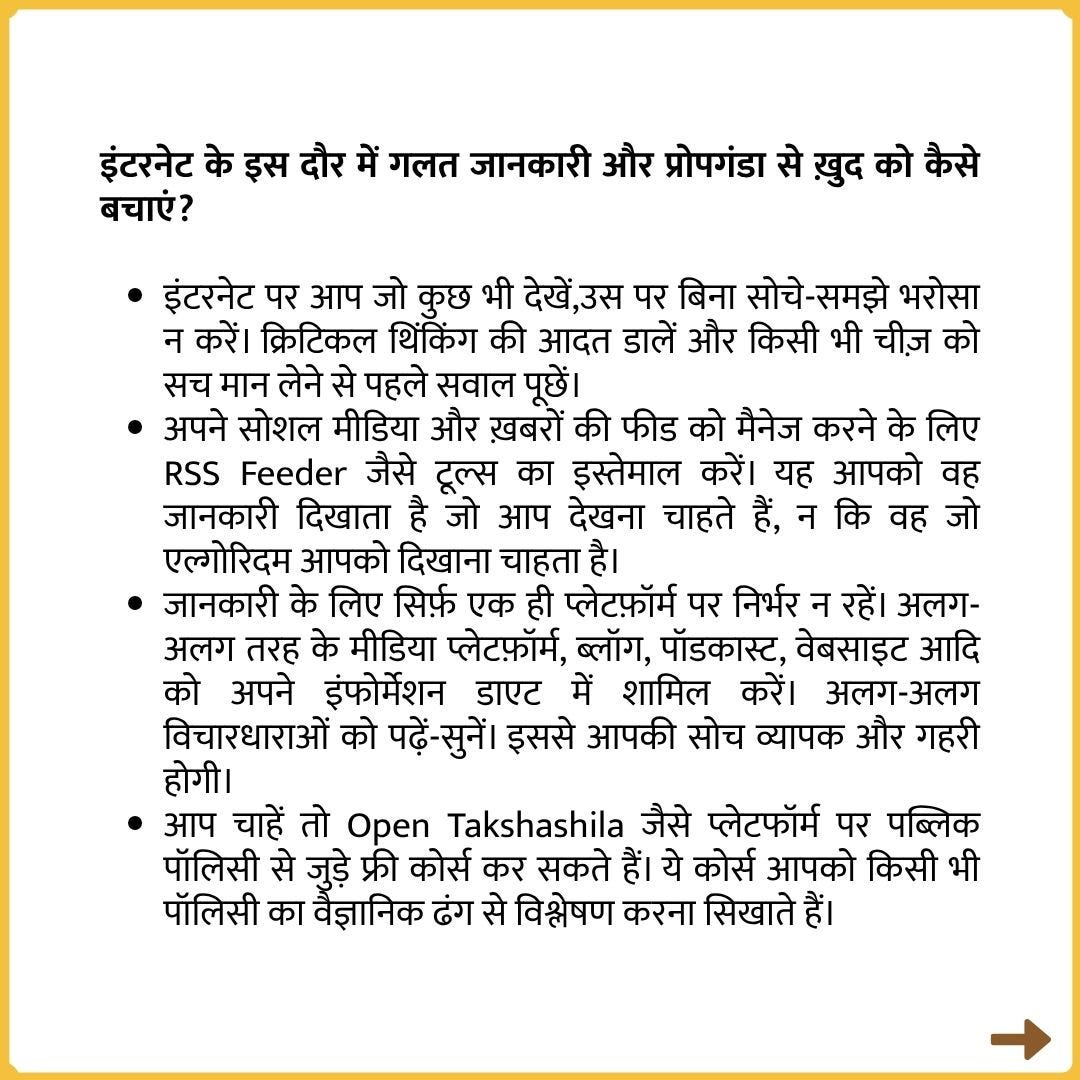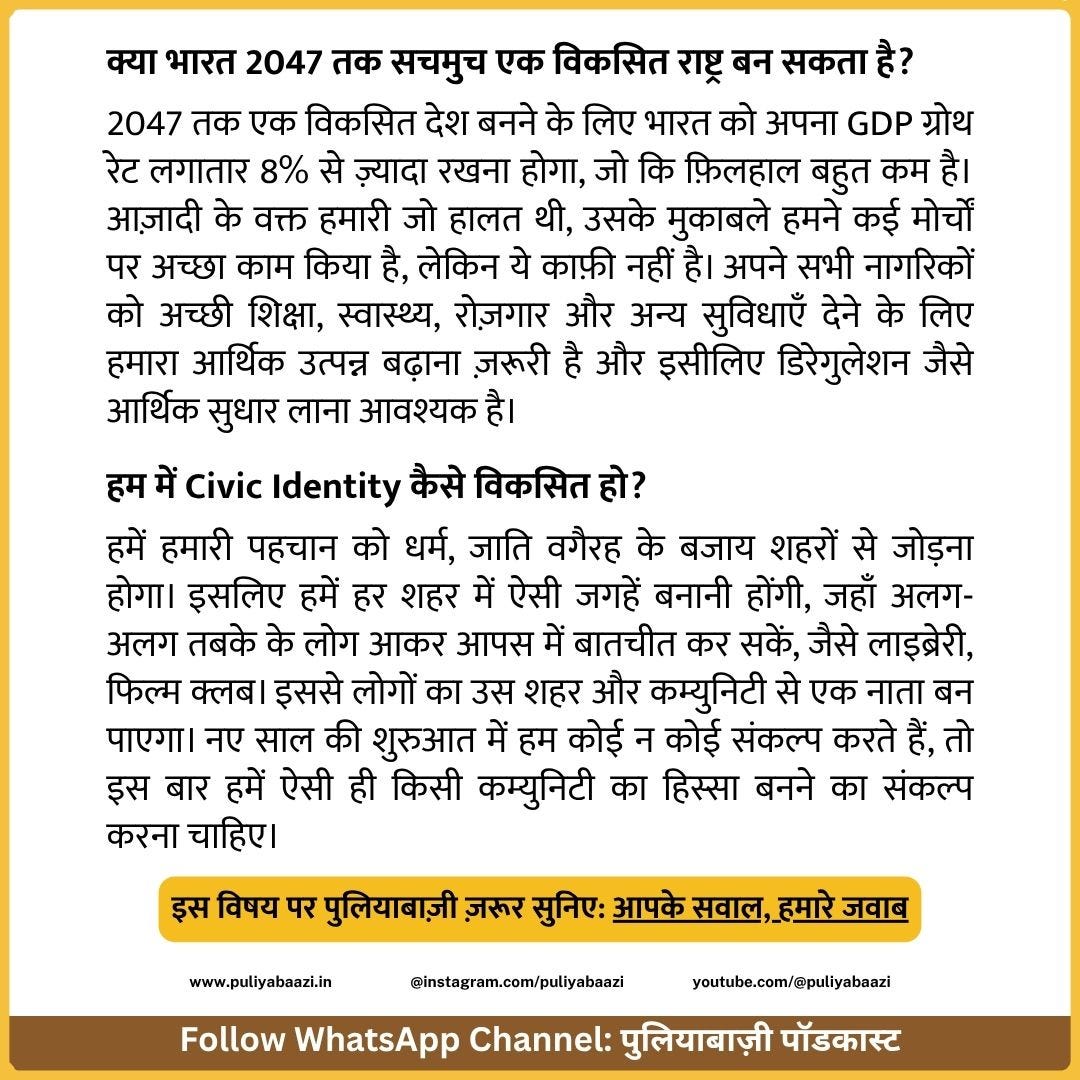मिल्टन की अनसुनी सलाह | Milton's Message to India
Milton Friedman's Memorandum to Govt. of India; Puliyabaazi Saptahik; Puliyabaazi Magazine
यह कहानी है 1955 की। भारत आज़ाद होकर कुछ ही साल हुए थे और हमें अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा तय करनी थी। हम पहली पंचवर्षीय योजना लागू कर चुके थे और दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी। इसी दौरान पं. जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से सलाह-मशवरे के लिए अपने अर्थशास्त्री भेजने की विनती की। इसे भारत को सोवियत रशिया के प्रभाव से छुड़ाने का मौका समझकर अमेरिका ने भी तुरंत अपने दो विद्वान अर्थशास्त्री भेज दिए, जिनमें से एक थे Neil Jacoby और दूसरे थे Milton Friedman।
फ़्रीडमैन लगभग एक महीना भारत में रहे और उन्होंने अपने अध्ययन तथा अनुभवों के आधार पर भारत सरकार को एक मेमोरेंडम लिखा। लेकिन सरकार ने उस वक्त इसे कोई अहमियत नहीं दी, न ही अगले साडेतीन दशकों तक यह प्रकाशित हो पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिल्टन का मेमोरेंडम तत्कालीन नीति के बिल्कुल विरुद्ध था। दरअसल, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण सरकारी नियंत्रण पर ज़ोर दिया गया था। मगर मिल्टन खुले बाज़ार और लोगों की आज़ादी के समर्थक थे। मिल्टन ने उस वक्त जो सुझाव दिए, वे इतने दूरदर्शी थे कि पैंतीस साल बाद, 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार हुए, तो हमने लगभग उन्हीं बातों को लागू किया। हालाँकि आज भी हम उनके सभी सुझावों को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं।
मिल्टन 1963 में दोबारा भारत आए थे और तब भी उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए थे, जिनका सार हमने पुलियाबाज़ी पर इस लेख में प्रकाशित किया है। हालाँकि मिल्टन का मेमोरेंडम भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्होंने कई और अहम सुधारों की भी बात की है।
तो आइए समझते हैं मिल्टन के मेमोरेंडम का सार।
तरक्की का राज़: पाबंदी नहीं, आज़ादी
फ़्रीडमैन अपने मेमोरेंडम की शुरुआत में ही लिखते हैं कि वार्षिक 5% विकास दर हासिल करना भारत के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल भारत में मौजूद है। सवाल सिर्फ़ यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? सरकारी नियंत्रण के ज़रिए इसका कारगर इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसा माहौल बनाए, जिसमें लोगों को अपनी सोच, समझ और क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करने की आज़ादी मिले।
यह लक्ष्य हासिल करने के लिए मिल्टन ने सरकार कुछ नीतिगत सुझाव दिए, पेश है उनका सार :
निवेश नीति
उस वक्त भारत सरकार में यह मान्यता थी कि जितना ज़्यादा निवेश होगा, उतना ही तेज़ विकास होगा। मिल्टन इस सोच को एक बड़ी भूल मानते हैं। वे कहते हैं कि एक तो निवेश कितना किया जाता है, उतना ही या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वह कहाँ और कैसे किया जाता है। दूसरी बात, किसी भी देश का विकास वहाँ की मशीनों और इमारतों से ज़्यादा वहाँ के इंसानों की काबिलियत पर निर्भर होता है। इसलिए निवेश सिर्फ़ भौतिक चीज़ों में नहीं, लोगों की क्षमता बढ़ाने में भी होना चाहिए।
मध्यम मार्ग का महत्व
भारत की तत्कालीन निवेश नीति दो विरुद्ध छोरों पर जोर देती थी। एक तरफ़ भारी उद्योगों में निवेश किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ़ कुटीर उद्योग और हस्तकला जैसे उद्योगों में। भारी उद्योगों में पूंजी ज़्यादा लगती थी पर रोज़गार कम बनते थे, जबकि कुटीर उद्योग में बहुत सारे लोग काम करते थे पर पूंजी कम लगती थी। मिल्टन का सुझाव था कि भारत को छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यही उद्योग भारी उद्योगों की नींव बनते हैं और बड़े पैमाने पर रोज़गार भी पैदा करते हैं।
पब्लिक सेक्टर की मर्यादा
मिल्टन कहते हैं कि भारत को हर चीज़ के राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण से बचना चाहिए। दूसरे महायुद्ध के बाद कई यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयकरण की होड़ लगी थी, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही निराशाजनक रहे। मिल्टन सलाह देते हैं कि भारत में सरकार के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा काम है और वह करने के लिए काबिल अधिकारियों की कमी है। इसलिए सरकार को वे सभी काम निजी क्षेत्र पर छोड़ देने चाहिए जिन्हें वह कर सकता है।
निवेश पर नियंत्रण से नुकसान
उस वक्त भारत में इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस-परमिट-कोटा सिस्टम था और इससे निवेश पर भी कई मर्यादाएँ आती थीं। इस नीति की खामियाँ दिखाते हुए मिल्टन कहते हैं कि,
सरकार कहती है इसलिए लोग कंपनी नहीं खोलते। अगर वे अपने पसंदीदा क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकते तो फिर वे अपने पैसे कहीं और खर्च करते हैं।
कौन सा निवेश सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा यह पहले से कोई नहीं जानता। इसलिए परिस्थिति के अनुसार निवेश में बदलाव की आज़ादी होना ज़रूरी है, जो तत्कालीन नीति में नहीं थी।
निवेश को लेकर बहुत सारे नियम होने से सरकारी बाबुओं की ताकत उन्हें लागू करने में ही खर्च हो जाती है और प्राइवेट क्षेत्र की उनसे बचने या बदलने में।
महँगाई पर नियंत्रण रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है लेकिन इसे निभाने का सबसे बेहतर ज़रिया है मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी है, न कि रेगुलेशन।
प्राइवेट सेक्टर के प्रति नीति
मैन्युफैक्चरिंग के अकुशल तरीकों को संरक्षण
फ़्रीडमैन सरकार की उन नीतियों की आलोचना करते हैं जो इनफ़िशियंट मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा दे रही थीं, जैसे फैक्ट्री में बने जूतों पर टैक्स लगाकर हाथ से बने जूतों को संरक्षण देना। उनका कहना था कि भारत की मूल समस्या यहाँ के मेनपावर का अकुशल उपयोग है। अकुशलता को संरक्षण देना कोई समाधान नहीं हो सकता, बल्कि यह तो लोगों के क्षमता और पूंजी दोनों की बर्बादी है। इस नीति से कुछ रोज़गारों को थोड़े समय के लिए संरक्षण मिल सकता है, लेकिन बहुत सारे संभावित रोज़गार उत्पन्न ही नहीं होंगे।
कहीं अत्यधिक छूट तो कहीं अत्यधिक नियंत्रण
मिल्टन का कहना था कि निजी उद्योगों को न तो विशेष रियायतें मिलनी चाहिए और न ही उन्हें बेवजह परेशान किया जाना चाहिए। कुछ प्राइवेट कंपनियों को आसान कर्ज़, मार्केट की गारंटी, और कीमत-निश्चित करने की अनुमति तथा उनके प्रतिस्पर्धियों को लाइसेंस नकारना—आदि जैसी नीतियों से कामचोरी बढ़ती है और संसाधनों की बर्बादी होती है। मिल्टन के अनुसार निजी क्षेत्र को स्पर्धा के माहौल में अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए। अगर किसी को मुनाफ़ा कमाना है, तो उसे घाटे का जोखिम भी उठाना चाहिए।
मॉनिटरी पॉलिसी
मिल्टन ने भारत सरकार को सबसे सख्त चेतावनी दी उसकी मॉनिटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति को लेकर। मिल्टन का मानना था कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक स्थिर मौद्रिक माहौल बेहद ज़रूरी है। उनका मानना था कि मॉनिटरी पॉलिसी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें की गई गलतियाँ सबसे ज़्यादा विनाशकारी साबित हो सकती है और सही नीति सबसे ज़्यादा लाभकारी।
अस्थिर मॉनिटरी पॉलिसी
मिल्टन ने पाया कि भारत की तत्कालीन मॉनिटरी पॉलिसी बहुत ही अस्थिर थी। कभी सरकार बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसा ले आती जिससे महँगाई बढ़ जाती, तो कभी बहुत सख्त रूख अपनाती जिससे मंदी आ जाती। उनका सुझाव था कि भारत को देश में उपलब्ध कुल पैसों पर ध्यान देना चाहिए और इसमें हर साल 4% से 6% तक की दर से बढ़ोतरी होने देनी चाहिए।
डेफ़िसिट फ़ाइनैंसिंग
उस वक्त भारत सरकार की कमाई और खर्च में बड़ा अंतर था, जिसे मिटाने के लिए सरकार हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए का डेफ़िसिट फ़ाइनैंसिंग कर रही थी, यानी कर्ज़ लेना, अतिरिक्त नोट छापना आदि के ज़रिए यह पैसे बना रही थी। मिल्टन ने चेतावनी दी कि सरकार अगर इसी दर से डेफ़िसिट फ़ाइनैंसिंग करती रही तो महँगाई 30% या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
उनका सुझाव था कि सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए इतने ज़्यादा टैक्स या नोट छापने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सबसे अच्छा यही है कि सरकारी योजनाओं का आकार ही कम किया जाए और जो काम निजी क्षेत्र कर सकता है वो उसे करने दिए जाएँ।
व्यापार घाटा और डॉलर की समस्या
उस समय भारत में डॉलर की कमी थी। आयात के लिए ज़्यादा डॉलर की चाहिए थे और निर्यात से उतनी कमाई नहीं हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने लाइसंस-कोटा-परिमट का एक पेचीदा सिस्टम बना रखा था। मिल्टन ने इसे भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा बताया और कहा यह सिस्टम अकुशलता, मनमानी और भ्रष्टाचार को जन्म देता है।
मिल्टन इस पर दो तरह के समाधान देते हैं :
विदेशी मुद्रा की नीलामी: सरकार जितनी विदेशी मुद्रा देना चाहती है, उसकी नीलामी करे। जिसे खरीदना है, वह बोली लगाए। हालाँकि यह सर्वोत्तम उपाय नहीं है, प्रचलित लाइसेंस राज से तो बेहतर है।
Floating Exchange Rate (लचीला विनियम दर): रुपए की कीमत सरकार तय न करे, बल्कि बाज़ार को तय करने दे। अगर डॉलर की माँग बढ़ेगी, तो रुपया अपने आप थोड़ा सस्ता हो जाएगा। इससे विदेशों में भारतीय वस्तुएँ सस्ती हो जाएँगी और निर्यात बढ़ेगा, वहीं विदेशी वस्तुएँ महँगी होने से आयात कम होगा। इस तरह डॉलर और आयात-निर्यात का संतुलन अपने आप होगा। इसलिए मिल्टन इसे सबसे बेहतर उपाय कहते हैं।
आगे मिल्टन यह भी कहते हैं कि डॉलर और व्यापार की समस्याओं को अलग-अलग समझना गलती है। दरअसल ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आयात बढ़ती है तो सिर्फ़ वस्तुएँ ही नहीं आती, साथ-साथ लोग भी आते हैं, संपर्क बढ़ता है। नए लोग व्यापार के नए अवसर खोजते हैं, जिससे व्यापार बढ़ता है, निवेश बढ़ता है और आखिर में सभी को लाभ होता है।
अंत में मिल्टन कहते हैं कि अपने मेमोरेंडम में उन्होंने आर्थिक और वित्तीय सुधारों पर सर्वाधिक ज़ोर दिया है क्योंकि भारत की नीति में सबसे बड़ी खामी इसी क्षेत्र में हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि भारत की असली चुनौती है—अपने लोगों की क्षमता बढ़ाना, उनमें उम्मीद जगाना, कठोर सामाजिक और आर्थिक बंधनों को कम करना तथा हर वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर और आज़ादी देना।
—Summary of Milton Friedman’s Memorandum to Government of India, 1955
संपादन: परीक्षित सूर्यवंशी
We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.
पुलियाबाज़ी साप्ताहिक
इस विषय पर पुलियाबाज़ी यहाँ सुन सकते हैं: आपके सवाल, हमारे जवाब
पुलियाबाज़ी मैगज़ीन!
पुलियाबाज़ी मैगज़ीन का काम अब अंतिम चरणों में पहुँच चूका है। हमारे पहले मैगज़ीन की थीम है ‘डिरेगुलेशन’। चूँकि आप पुलियाबाज़ी के पाठक हैं, डिरेगुलेशन का महत्व तो आप जानते होंगे, फिर भी यह मैगज़ीन आपको इस प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित कराएगी। हमें उम्मीद है आपको हमारी मैगज़ीन पसंद आएगी।
और यह उम्मीद भी है कि आपने अपनी फ्री कॉपी बुक कर ली होगी? अगर नहीं तो तुरंत इस लिंक पर अपना नाम और पता दर्ज कीजिए, क्योंकि पहली फ्री 500 कॉपीज जल्द ही खत्म वाली हैं!