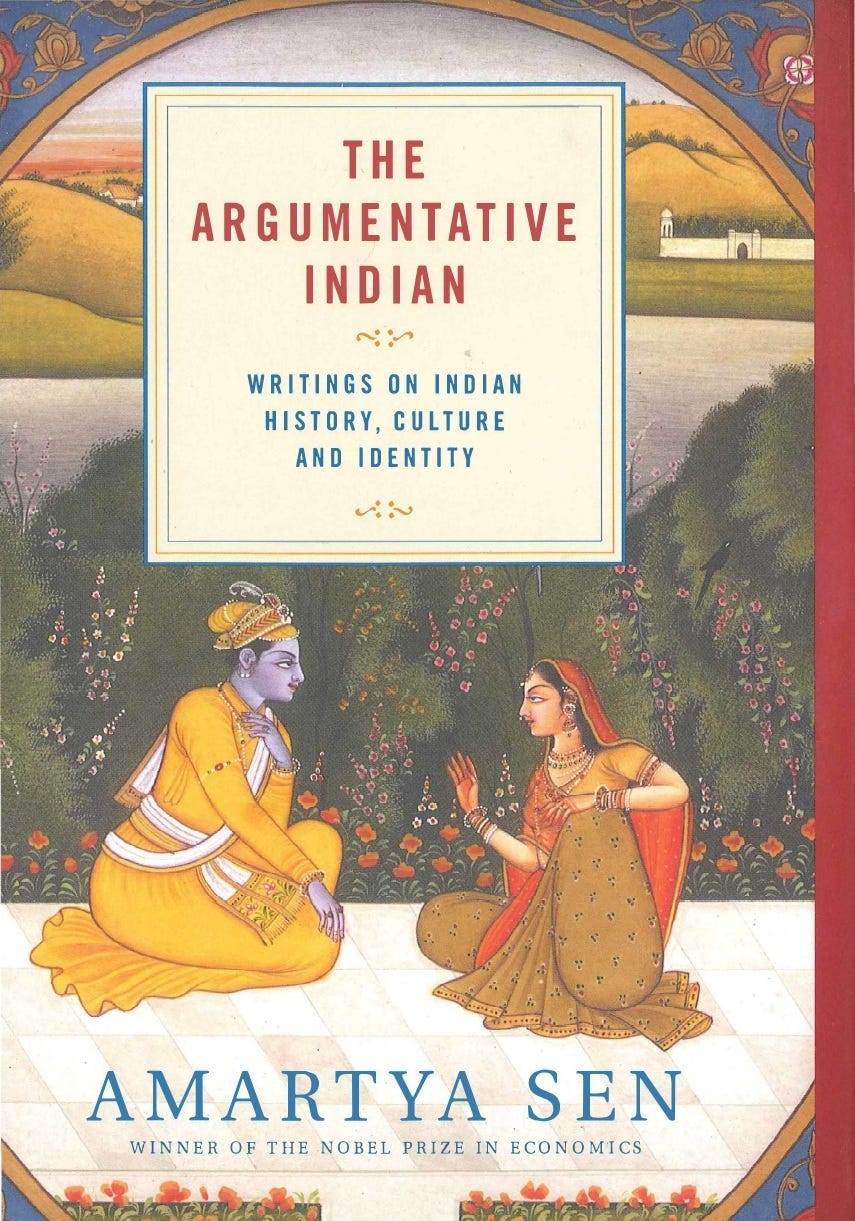भारत को अक्सर एक धार्मिक, विज्ञान-विरोधी और परंपराओं में जकड़ा हुआ देश माना जाता है। परंतु प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन अपनी किताब ‘The Argumentative Indian’ में हमें भारत के एक अलग रूप से परिचित करवाते हैं। भारत एक विवेकी, विचारशील देश है। यहाँ वाद, विवाद और संवाद की एक प्राचीन परंपरा रही है, जो केवल धर्म और अध्यात्म में ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन के हर आयाम में देखी जा सकती है।
वैसे तो प्रो. सेन की इस किताब में कई अध्याय हैं और वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक छोटे से लेख में इन सभी अध्यायों पर चर्चा करना संभव नहीं है। इसलिए आइए हम इस किताब के पहले अध्याय, ‘The Argumentative Indian’ को सारांश रूप में समझते हैं।
भारत में वाद-विवाद की प्राचीन परंपरा
भारत ने विश्व को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, महाभारत दिया है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जिसे इस काव्य ने स्पर्श नहीं किया। वाद-विवाद और चर्चाओं से भरा महाभारत, भारत की तर्कशील परंपरा का प्रतीक है। इसमें निहित विवादों की गुणवत्ता और गहराई भी बहुत व्यापक है। पूरे विश्व में सराही जाने वाली भगवद्गीता भी इसी का हिस्सा है। गीता मूलतः श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ विवाद है। इसमें अर्जुन रणभूमि में अपनों को मारने की कल्पना से व्यथित होकर युद्ध त्यागने की बात करते हैं ओर कृष्ण उन्हें कर्तव्यपालन की अहमियत समझाते हैं।
हालाँकि महाभारत में अर्जुन श्रीकृष्ण की बात मान लेते हैं और युद्ध करते हैं, प्रो. सेन अर्जुन के पक्ष को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमें भी हमारे कर्मों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। लेखक यह भी कहते हैं कि विवाद में सिर्फ़ विजेता पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं होता, दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए महाभारत में अर्जुन के पक्ष को भी विस्तार से दर्ज किया गया है।
तर्कशीलता और समानता
भारत की तर्कशील परंपरा पर एक अहम आक्षेप यह लिया जाता है कि इसपर उच्च जाति के पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। इसपर अमर्त्य सेन कहते हैं कि हालाँकि भारत में लिंग, वर्ग, जाति आदि के आधार पर काफ़ी भेदभाव होता आया है, इन वर्गों ने इन बंधनों के बावजूद वाद-विवाद में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।
महिलाओं की बात करें तो भारत के सामाजिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता विश्व के अन्य देशों से कहीं ज़्यादा रही है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच हुई बहस को प्राचीन भारत की सबसे गहन अध्यात्मिक चर्चाओं में से एक माना जाता है। इसी तरह रामायण में सीता और महाभारत में द्रौपदी एक मज़बूत किरदार के रूप में उभरकर आती हैं। सिर्फ़ प्राचीन ही नहीं, आधुनिक काल में भी भारतीय महिलाएँ उतनी ही सशक्त रही हैं। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, जबकि मार्गरेट थेचर उनके पचास साल बाद 1975 में ब्रिटेन के एक बड़े राजनीतिक पक्ष की अध्यक्ष बनीं।
भारत की तर्कशील परंपरा ने जाति और वर्ग के बंधनों को भी कई बार लाँघ दिया है। भारत में जब ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व बढ़ गया तब बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ और चूँकि इन धर्मों में समानता को काफ़ी अहमियत दी गई, इनका प्रचार-प्रसार भी बहुत तेज़ी से हुआ। महाभारत में भृगु और भारद्वाज के संवाद से लेकर कबीर, दादू, रविदास, सेना महाराज और मीरा बाई तक, भारत में हर वर्ग और जाति के व्यक्तियों ने तर्क की इस परंपरा का पोषण किया है।
लोकतंत्र का आधार
लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र की नींव ब्रिटिशों द्वारा रखी गई, लेकिन भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही है। ब्रिटेन की सत्ता तो भारत सहित कई अन्य देशों में थी, लेकिन सभी में लोकतंत्र नहीं पनप पाया, इसकी एक वजह यह भी है कि भारत में मूलतः लोकतंत्र की जड़ें पहले से मौजूद थीं।
लेखक कहते हैं हमें इन दोनों ही निष्कर्षों से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक चर्चा की परंपरा विश्व के सभी देशों में कम-ज़्यादा रही है। जहाँ यह परंपरा जितनी मज़बूत रही वहाँ लोकतंत्र स्थापित करना और कायम रखना उतना ही आसान रहा।
दरअसल, वाद-विवाद और संवाद लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ वोट देना ही नहीं होता। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए लोगों का राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होना भी उतना ही ज़रूरी होता है।
वाद-विवाद और धर्मनिरपेक्षता
अमर्त्य सेन कहते हैं कि वाद-विवाद की इस परंपरा ने भारत में न सिर्फ़ लोकतंत्र की स्थापना में, बल्कि इसे एक धर्मनिरपेक्ष (secular) देश बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई जैसे कई धर्मों और जातियों के लोग यहाँ सदियों से एक साथ रहते आए हैं।
लेखक ने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने में बहुत बड़ा योगदान देनेवाली दो महान हस्तियों का ज़िक्र किया है—सम्राट अशोक और बादशाह अकबर। सम्राट अशोक ने विवाद में भी वाणी पर संयम बरतने की आज्ञा दी थी। उनका कहना था कि आप भले ही अन्य संप्रदाय की कोई एक बात पसंद नहीं करते, लेकिन उनमें और कई बातें हो सकती हैं जिनके लिए आपको उनका आदर करना चाहिए। अशोक की यह आज्ञा बुद्ध के उस विचार से प्रेरित थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि,
"जो व्यक्ति अपने संप्रदाय (धर्म) के प्रति मोह के कारण, सिर्फ़ अपने ही संप्रदाय का आदर करता है और दूसरों के संप्रदायों की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने ही संप्रदाय को सबसे अधिक हानि पहुँचाता है।"
अकबर के बारे में लेखक कहते हैं कि अकबर ने आधुनिक भारत में धर्मनिरपेक्ष, क़ानून-आधारित राज्य की नींव रखी। अकबर धार्मिक सहिष्णुता को सर्वोपरि मानते थे। उनके राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य था—'किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के कारण परेशान नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना पसंदीदा धर्म अपनाने की आज़ादी होगी।'
अकबर के दरबार में कई धर्म के विद्वान और कलाकार थे। वह अक्सर सार्वजनिक चर्चाओं का आयोजन करते थे जिसमें सभी धर्म के विद्वान वाद-विवाद करते थे। अकबर के सेनापति भी एक हिंदू थे, राजा मान सिंह जिन्हें अकबर पहले युद्ध में हराया था। हालाँकि अकबर से पहले भी भारत में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता की लंबी परंपरा रही है, अकबर के समय में इसे ज़बरदस्त बढ़ावा मिला।
अज्ञेयवाद और नास्तिकता
भारत में सिर्फ़ धार्मिक विचारों को ही नहीं, अज्ञेयवादी, नास्तिकवादी और भौतिकवादी विचारों को भी उतनी ही अहमियत दी गई है। ईसा पूर्व दो हज़ार साल पुराने ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में संदेहवादी विचार व्यक्त किए गए हैं। यही परंपरा आगे भी कायम रही है। आपको शायद यकीन न हो लेकिन संस्कृत में धार्मिक साहित्य के साथ ही अज्ञेयवादी और नास्तिकवादी साहित्य अन्य किसी भी भाषा से अधिक है!
ईश्वर और परलोक को न माननेवाले चार्वाक इसी भारत में हुए। उन्होंने ‘लोकायत’ दर्शन के माध्यम से भौतिकवादी विचारों का प्रसार किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि,
यावज्जीवेत्सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ।।
(जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो, श्मशान में शरीर के भस्म होने पर पुनर्जन्म कैसे होगा?)
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थनीति और शासन पर चर्चा की। इसमें धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मानपूर्वक उल्लेख ज़रूर है, परंतु वास्तव में यह एक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है।
वाद-विवाद और विज्ञान
ज्ञान और विज्ञान का वाद-विवाद से करीबी संबंध है। कोई भी नया आविष्कार पुराने विचारों से अलग, नए विचार से ही जन्म लेता है। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन और डार्विन—सभी ने विश्व को नए सिद्धांत दिए जो प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देते थे। भारत में भी विज्ञान के विकास में इस परंपरा का बड़ा योगदान रहा।
विचारों के आदान-प्रदान और निरीक्षण की इसी परंपरा के कारण भारतीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ बेबिलोन, ग्रीस और रोम से काफ़ी कुछ सीख पाए और उन्होंने उस ज्ञान का उपयोग भारतीय खगोलशास्त्र में किया। इसी तरह भारतीय गणित और खगोलशास्त्र से अरबी और ईरानी वैज्ञानिकों ने सीखा।
भारत में विज्ञान और गणित का विकास मुख्य रूप से गुप्त काल में हुआ। पाँचवीं शताब्दी में आर्यभट, छठी में वराहमिहिर और सातवीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने इस क्षेत्र में अमूल्य कार्य किया। आर्यभट के ग्रंथ ‘आर्यभटीय’ ने भारत ही नहीं, अरब में भी बड़ी खलबली मचा दी थी। आर्यभट ने नए सिद्धांतों तो प्रस्तुत किए ही, साथ ही प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को सिरे से ख़ारिज करते हुए उनका पुरजोर विरोध किया। उस काल में यह सब करना किसी क्रांति से कम नहीं था। दुर्भाग्य से, आर्यभट के बाद आए ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने उतनी हिम्मत नहीं दिखाई।
ग्यारहवीं सदी के ईरानी खगोलशास्त्री अलबिरूनी, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त के संस्कृत प्रबंध ब्रह्मसिद्धांत का अरबी अनुवाद किया, कहते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने धार्मिक रूढ़िवादियों को खुश रखने के लिए आर्यभट की आलोचना की, लेकिन आर्यभट की ही वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते रहें।
हालाँकि अलबिरूनी ब्रह्मगुप्त को अपने समय के सबसे महान गणितज्ञ और आर्यभट जितने ही (या उनसे भी बड़े) विद्वान मानते थे, ब्रह्मगुप्त के इस दोहरे रवैये से निराश थे। उन्हें लगता था कि ब्रह्मगुप्त आर्यभट जितने निडर और क्रांतिकारी नहीं थे।
अलग सोच रखने की हिम्मत और असहमति जताने की ताक़त विज्ञान में भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि समाज में लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत करने के लिए।
वाद-विवाद और संवाद का महत्व
अध्याय के अंत में प्रो. अमर्त्य सेन यह बात साफ़ करते हैं कि भारत को समझने के लिए बेशक सिर्फ़ उसकी ‘वाद-विवाद की परंपरा’ समझना काफ़ी नहीं है, इसके और भी कई पहलू समझने होंगे, लेकिन भारत को हमेशा से एक बहुत ही धार्मिक, विज्ञान-विरोधी, रूढ़िवादी देश मान लेना भी उचित नहीं है।
राजनीति और विज्ञान से लेकर साहित्य तक यह परंपरा चलती आई है और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए इस परंपरा को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। रबिंद्रनाथ टैगोर अपने काव्य में ईश्वर से यही तो माँगते हैं,
Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by narrow
domestic walls; . . .
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert
sand of dead habit; . . .
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake
अध्याय को समाप्त करते हुए प्रो. सेन राजा राममोहन राय की एक पंक्ति साझा करते हैं,
Just consider how terrible the day of your death will be.
Others will go on speaking, and you will not be able to argue back.
असहमति, तर्क और वाद-विवाद की यह विरासत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। हमें इसे अपनाना और बचाए रखना चाहिए क्योंकि इससे ही भारत का विकास संभव है।
—अमर्त्य सेन की किताब The Argumentative Indian के पहले अध्याय का सारांश
संपादन—परीक्षित सूर्यवंशी
प्रो. अमर्त्य सेन की किताब आप यहाँ पा सकते हैं:The Argumentative Indian
We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.