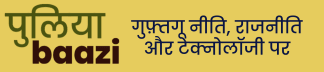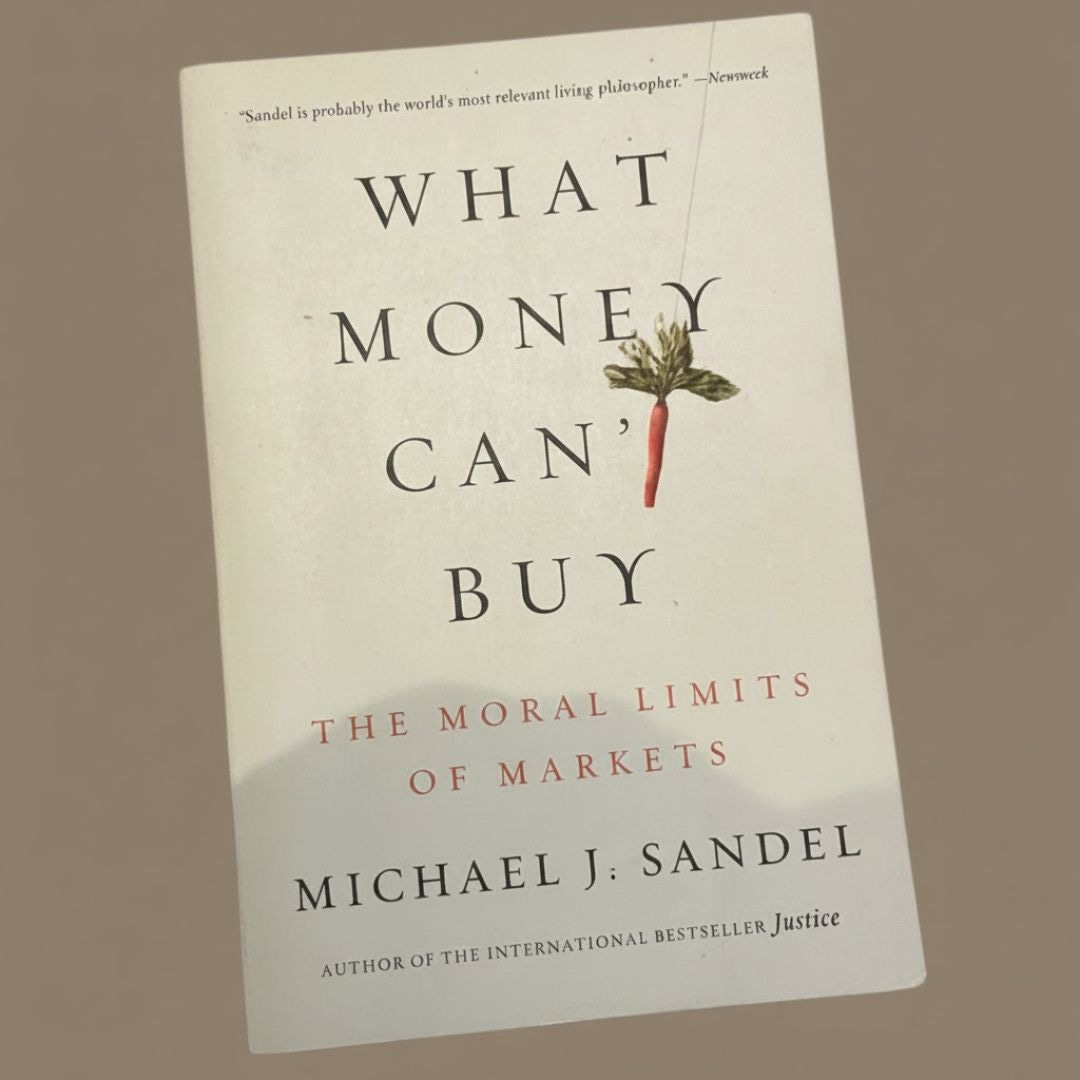मार्केट की मर्यादा कहाँ तक? । Moral Limits of Markets
A review of Prof. Michael Sandel's book 'What Money Can't Buy: Moral Limits of Markets'
अगर आप फिलोसोफी में दिलचस्पी रखते हैं तो शायद आपने Prof. Michael Sandel का नाम सुना होगा। माइकल सैंडेल हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल फिलोसोफी के प्रोफ़ेसर तथा अमरीका के जाने-माने बुद्धिजीवियों में से एक हैं। नैतिकता, न्याय और तर्क पर हार्वर्ड में ही दी गई उनकी लेक्चर सीरीज़, Justice: What’s the Right Thing to Do? दुनियाभर के जिज्ञासुओं में अत्यंत लोकप्रिय है। श्रोताओं के साथ सवाल-जवाब करते हुए अपना विषय समझाने की उनकी सोक्रेटिक शैली सुननेवाले को बाँधे रखती है।
इन्हीं प्रो. माइकल सैंडेल की एक किताब है, ‘What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets’ जो समाज और बाज़ार की भूमिकाओं पर प्रकाश डालती है। हम भी अक्सर समाज, सरकार और बाज़ार की बात करते हैं। यह किताब पढ़कर मेरे दिमाग में इनके परस्पर संबंधों के बारे में थोड़ी और स्पष्टता आई। तो आइए, इस हफ़्ते इसी पर बात करते हैं।
आजकल बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकतीं। किताब में दिए गए कुछ उदाहरण देखिए, कुछ अमरीकी जेलों में लगभग 90 डॉलर देकर कैदी अपने लिए एक अलग, साफ़-सुथरा कमरा ले सकते हैं, भीड़ के समय अकेले कार चालक 8 डॉलर देकर शेयरिंग-कार की लेन में चल सकते हैं, यूरोप में कोई भी कंपनी 18 डॉलर देकर एक मेट्रिक टन कार्बनडाई ऑक्साइड हवा में छोड़ सकती है। ये उदाहरण शायद आपको थोड़े अजीब लगें, लेकिन ऐसे कई क्षेत्रों में आज बाज़ार प्रवेश कर रहा है जहाँ पर वह पहले नहीं था। इसे प्रो. माइकल ‘मार्केट ट्रायम्फ़लिज़्म’ कहते हैं। ऐसे में हमारे लिए यह सोचना ज़रूरी हो जाता है कि समाज में पैसों की भूमिका क्या होनी चाहिए।
“The era of market triumphalism has come to an end. The financial crisis did more than cast doubt on the ability of markets to allocate risk efficiently. It also prompted a widespread sense that markets have become detached from morals and that we need somehow to reconnect them.”
ज़रा सोचिए और बताइए कि क्या किताब पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे देने चाहिए? टेक्सास के एक स्कूल में एक प्रयोग किया गया। एक किताब पढ़ने पर बच्चों को 2 डॉलर दिए गए। अर्थशास्त्र सिखाता है कि इंसान इंसेंटिव के अनुसार काम करता है। इसलिए अगर कुछ बच्चों की पढ़ने में रुचि नहीं है, तो उन्हें प्रेरित करने के लिए पैसों का इंसेंटिव के तौर पर इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? हो सकता है इससे बच्चों को पढ़ने की आदत लग जाए।
लेकिन यह भी हो सकता है कि इससे बच्चों में पढ़ने की प्रेरणा बदल जाए, वे किताब पढ़ने को पैसे कमाने का ज़रिया समझ लें, न कि ज्ञान और आनंद पाने का। हो सकता है इससे किताबों के चुनाव पर भी असर पड़े (जैसे टेक्सास में कई बच्चों ने छोटी किताबें चुनी)। लेकिन यह तो हमारा मकसद नहीं था!
प्रोफेसर सैंडल इसे ‘Crowding Out Effect’ कहते हैं, यानी जहाँ पर पैसों का काम नहीं है, वहाँ पर पैसों के आने से हमारा असली मकसद धुंधला हो सकता है और हम भटक सकते हैं।
एक और उदाहरण देखते हैं। अमरीका में लाइन-स्टेंडिंग यानी कतार में खड़े रहने के लिए लोग मुहैया करानेवाली बाकायदा कंपनियाँ है। ये कंपनियाँ बेघर और गरीब लोगों को लाईन में खड़े रहने के लिए 10-20 डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से पैसे देती हैं। जब वहाँ कांग्रेस की सुनवाई (Congressional hearing) होती है तो लॉबिस्ट खुद लाइन में खड़े रहने के बजाय इन कंपनियों से टिकट खरीदते हैं, जो 1000 डॉलर या उससे महँगें हो सकते हैं। इस तरह वे तो सभा में घुस जाते हैं लेकिन वो लोग बाहर रह जाते हैं, जो इतनी रकम नहीं दे सकते। बेशक हम कह सकते हैं कि इन लोगों को अगर सभा में शामिल होना इतना ही महत्वपूर्ण लगता है तो वे भी उन गरीबों की तरह रातभर लाइन में क्यों खड़े नहीं रहते? लेकिन हमें अपनेआप से यह भी पूछना चाहिए कि जिस तरह हम किसी क्रिकेट मैच का टिकट खरीदते हैं उसी तरह कांग्रेस की सभा का टिकट लेकर किसी का उसमें शामिल होना, क्या एक समाज के तौर पर हमें सही दिशा में ले जाता है?
यहाँ यह बात साफ़ कर दें कि माइकल सैंडेल कोई मार्क्सवादी नहीं हैं, न ही वे खुले बाज़ार के खिलाफ़ हैं। दरअसल भौतिक चीज़ों की लेन-देन में बाज़ार की अहमियत को वे अच्छी तरह समझते हैं। वे कहते हैं कि
“As the cold war ended, markets and market thinking enjoyed unrivaled prestige, understandably so. No other mechanism for organizing the production and distribution of goods had proved as successful at generating affluence and prosperity.”
वे सिर्फ़ इतना कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में बाज़ार जीवन के उन क्षेत्रों में घुस गया है, जहाँ उसकी जगह नहीं है। वे पूछते हैं कि क्या हम ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जहाँ सामाजिक नैतिकता, इंसानी रिश्ते, राजनीति और कानून जैसी चीज़ों की भी विशिष्ट कीमत हो? जहाँ जीवन के हर एक पहलू पर पैसों का राज हो?
“We drifted from having a market economy to being a market society. The difference is this: A market economy is a tool—a valuable and effective tool—for organizing productive activity. A market society is a way of life in which market values seep into every aspect of human endeavor.”
सैंडेल कहते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में बाज़ार के आने से दो तरह का नुकसान हो सकता है। एक तो समाज के कमज़ोर तबके पर अन्याय हो सकता है और दूसरा जिस चीज़ की कीमत लगाई जाती है उसका पतन हो सकता है। जैसे इज़राइल में एक डे-केयर सेंटर ने नियम लागू किया कि जो माँ-बाप बच्चों को लेने के लिए देरी से आएँगे उन पर दण्ड लगाया जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि देरी से आनेवालों की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई। लोगों ने दण्ड की रकम को लेट आने की फ़ीज मान लिया और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी न निभाने का दुःख भी नहीं हुआ। विशेष बात तो यह है कि दण्ड का नियम बंद करने के बाद भी माता-पिता का देरी से आना कम नहीं हुआ! यानी एक तरह से इंसानी रिश्ते और ज़िम्मेदारी का मूल्य गिर गया।
इस किताब के ज़रिये प्रो. सैंडल की कोशिश यह है कि हमारे नागरिक जीवन के बुनियादी सिद्धांतों को समझने के लिए पब्लिक डिबेट यानी सार्वजनिक विमर्श शुरू हो। खुले बाज़ार और अर्थव्यवस्था की अहमियत समझना जितना ज़रूरी है, उतना ही बाज़ार की नैतिक सीमाओं को पहचानना भी आवश्यक है। ऐसा करने से ही शायद हम एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।
एक सभ्य समाज में पैसे की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए यह दर्शाने के लिए सैंडेल वास्तविक जीवन से जुड़े कई उदाहरण देते हैं। वे इन उदाहरणों को तर्क और विवेक की कसौटी लगाते हैं और लोकतंत्र-नागरिकों के बीच बने सामाजिक करार का सार पेश करते हैं। मुझे यह किताब अहम लगती है क्योंकि, पब्लिक पॉलिसी के एक विद्यार्थी के नाते यह मुझे समाज और बाज़ार की उन मर्यादाओं को समझने में मदद करती है, जिनके धुंधलाने से अक्सर सामाजिक संघर्ष पैदा होता है। यह हमें अपने आप से यह सवाल पूछने को मजबूर करती है कि हम कैसे समाज में रहना चाहेंगे—सिर्फ़ पैसों के आधार पर चलनेवाले या नियमों के आधार पर चलनेवाले?
इसे पढ़कर हम में से कुछ लोगों को तो मास्टरकार्ड का वह विज्ञापन ज़रूर याद आएगा, “There are some things money can’t buy; for everything else, there’s Mastercard”
—परीक्षित
We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.
Best of 2025
पुलियाबाज़ी पर बातें करते-सुनते हम 2025 के आखिरी महीने में पहुँच गए। तो हमने सोचा क्यों न इस साल के कुछ खास एपिसोड, जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आपके साथ फिर एक बार शेयर करें। तो पेश है Best of Puliyabaazi 2025!