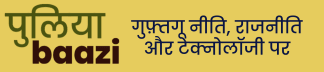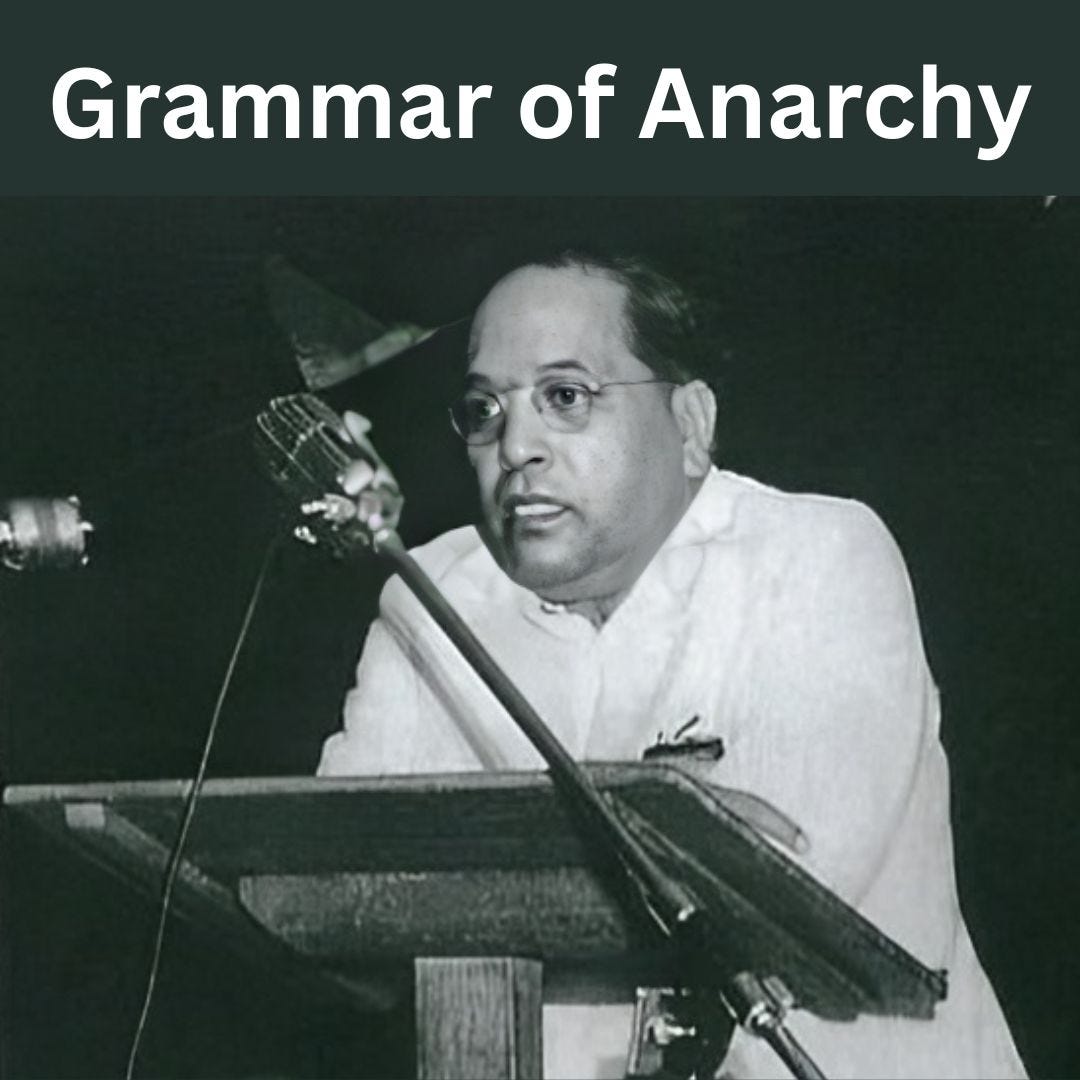अराजकता का व्याकरण
Grammar of Anarchy - Dr. Babasaheb Ambedkar's last speech in the constituent assembly, November 25, 1949.
The constituent assembly of India, formed in 1946, completed its work and submitted the Constitution of India with 395 articles, eight schedules and 22 parts to the parliament. The Constitution was adopted on November 26, 1949. A day before this momentous accession, the architect of the Indian Constitution, Dr Babasaheb Ambedkar, delivered a powerful speech in the parliament, which came to be known as the ‘Grammar of Anarchy’ speech.
As we celebrate his birth anniversary today, what would be a better tribute than to study and understand his thoughts on his country?
‘अराजकता का व्याकरण’ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिया गया अंतिम भाषण था। इसे पढ़कर हम समझ सकते है कि बाबासाहब के मन में भारत के लिए कितना प्रेम और चिंता थी। जिन चिंताओं ने उस वक्त उन्हें बेचैन कर रखा था वह आज भी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है।
आइए आज बाबासाहब की जयंती के अवसर पर फिर एक बार उनका वह हृदयस्पर्शी भाषण पढ़ते हैं और इस देश के प्रति उनके विचारों को कुछ हद तक समझने की कोशिश करते हैं।
हिंदी अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी
संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो बेशक संविधान भी बुरा ही साबित होगा। और कोई संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे होंगे तो वह अच्छा साबित होगा।
संविधान के पक्ष में जो कुछ कहा जा सकता था, वह सब मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री टी. टी. कृष्णमाचारी कह चुके हैं, इसलिए मैं संविधान के गुणों की चर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान भी बुरा ही साबित होगा। और कोई संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे होंगे तो वह अच्छा साबित होगा। संविधान की सफलता केवल उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं है। संविधान तो सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगों का ढांचा प्रदान करता है। लेकिन इन अंगों की कार्यक्षमता तो लोग और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा चुनी गई पार्टियाँ तय करती हैं।
आज यह कौन बता सकता है कि भारत के लोग और उनकी पार्टियाँ कैसा आचरण करेंगी? क्या वे अपना लक्ष्य पाने के लिए संवैधानिक पथ अपनाएंगी या फिर क्रांतिकारी मार्ग पसंद करेंगी? अगर वे क्रांतिकारी मार्ग चुनेंगी, तो फिर चाहे संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह कहने के लिए किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं कि वह विफल हो जाएगा। इसलिए लोग और उनकी पार्टियों की जिम्मेदारी के बारे में बात किए बगैर संविधान की सफलता और असफलता पर बहस करना व्यर्थ है।
संविधान की आलोचना मुख्यतः दो पक्षों द्वारा की जा रही है — कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी। वे संविधान की आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह एक खराब संविधान है? मेरा मानना है — नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा संविधान चाहती है जो ‘मजदूर वर्ग की तानाशाही’ (Dictatorship of the Proletariat)’ के सिद्धांत पर आधारित हो। वे संविधान की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र (parliamentary democracy) पर आधारित है।
समाजवादी दो चीजें चाहते है—पहली, अगर वे सत्ता में आएं तो संविधान उन्हें यह स्वतंत्रता दे कि वे बिना किसी मुआवजे के निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण कर सकें। और दूसरी, वे चाहते हैं कि संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार निरपेक्ष और निरंकुश हों, ताकि अगर वे सत्ता में न भी आएं, तो भी उन्हें सिर्फ आलोचना करने की ही नहीं, बल्कि राज्य को उखाड़ फेंकने तक की पूरी छूट मिले।
यही वे मुख्य कारण हैं जिनके आधार पर संविधान की आलोचना की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय लोकतंत्र ही राजनीतिक लोकतंत्र का एकमात्र आदर्श रूप है। मैं यह भी नहीं कहता कि निजी संपत्ति के अधिग्रहण के बदले मुआवजा देना इतना पवित्र सिद्धांत है कि उसे किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। और न ही मैं यह कहता हूँ कि मूलभूत अधिकार कभी भी निरंकुश नहीं हो सकते या उन पर जो मर्यादाएं लगाई गई हैं, उन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता। मैं तो बस यह कहना चाहता हूँ कि संविधान में जो सिद्धांत हैं वे वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं, और अगर यह भी आपको अतिशयोक्ति लगती है तो आप कह सकते हैं कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं। इन्हें संविधान में शामिल करने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी को दोष क्यों दिया जाए? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संविधान सभा के सदस्यों तक को क्यों दोष दिया जाए?
अमेरिका का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले महान नेता जेफरसन ने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिन्हें संविधान बनाने वाले कभी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। एक जगह वे कहते हैं:
“हम हर पीढ़ी को एक अलग क़ौम मान सकते हैं, जिसे बहुमत की इच्छा से खुद को बाँधने का अधिकार तो है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बाँधने का कोई अधिकार नहीं है—ठीक वैसे ही जैसे एक देश को किसी दूसरे देश के नागरिकों को बाँधने का अधिकार नहीं है।”
अन्य एक जगह जेफरसन कहते हैं:
“यह कहना कि राष्ट्र के लिए स्थापित संस्थाओं को छुआ या बदला नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें चलाने वाले व्यक्तियों को जनता के विश्वास से कुछ अनावश्यक विशेषाधिकार प्राप्त हैं शायद किसी राजा की मनमानी रोकने के लिए तो एक सुरक्षात्मक उपाय हो सकता है, लेकिन एक राष्ट्र के लिए तो यह एकदम बेतुकी बात है।
फिर भी हमारे वकील और पंडित इस विचार को फैलाते रहते हैं कि जैसे पिछली पीढ़ियों को हमसे ज़्यादा स्वतंत्रता थी, उन्हें हम पर ऐसे कानून थोपने का अधिकार था जिन्हें हम खुद भी नहीं बदल सकते, और उसी तरह से हम भी आज ऐसे कानून बना सकते हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां नहीं बदल सकती। संक्षेप में कहें तो ये ऐसा है जैसे कि इस पृथ्वी पर जिंदा लोगों का नहीं, बल्कि मुर्दों का हक़ है!"
मुझे लगता है कि जेफरसन ने जो कहा है वह सिर्फ सत्य ही नहीं बल्कि पूर्ण सत्य है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अगर संविधान सभा इस सिद्धांत से विचलित हो जाती तो वह जरूर दोषी ही नहीं, निंदा की पात्र भी होती। लेकिन मैं पूछता हूँ—क्या ऐसा हुआ है? बिलकुल नहीं। आप बस एक बार संविधान के संशोधन (amendment) से जुड़ी प्रक्रिया को देख लीजिए। हमारी संविधान सभा ने कनाडा की तरह नागरिकों को संविधान में संशोधन के अधिकार से वंचित नहीं किया है, ना ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह संशोधन के लिए असाधारण शर्तें लगाईं हैं। उलटा उसने संविधान संशोधन के लिए एक बहुत ही आसान प्रक्रिया प्रदान की है। मैं संविधान के आलोचकों को चुनौती देता हूं कि वे यह साबित करके दिखाएं कि दुनिया के किसी भी देश की संविधान सभा ने संविधान में संशोधन के लिए इतनी सरल प्रक्रिया का प्रावधान किया हो।
जो लोग संविधान से संतुष्ट नहीं हैं उन्हें संसद में बस दो-तिहाई (2/3) बहुमत हासिल करना है और अगर वे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं जुटा सकते तो इसका मतलब है कि उनका यह असंतोष आम जानता का असंतोष नहीं है।
मेरे हिसाब से संवैधानिक महत्व का केवल एक ही विषय है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक गंभीर शिकायत यह की गई है कि संविधान में केंद्रीकरण पर अत्यधिक जोर दिया गया है और राज्यों को मात्र नगरपालिका बना दिया गया है। यह बात तो साफ़ है कि यह विचार न केवल बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, बल्कि संविधान के उद्देश्य के बार में ही ग़लतफ़हमी दर्शाता है। जहाँ तक केंद्र और राज्यों के संबंध का सवाल है, यह समझना जरूरी है कि यह किस बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। संघवाद (federalism) का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी (legislative) और कार्यकारी (executive) अधिकारों का बँटवारा किसी केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। यही काम हमारा संविधान करता है।
हमारे संविधान में राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकारों के लिए किसी भी तरह केंद्र पर निर्भर नहीं हैं। इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों समान हैं। यह समझना सचमुच मुश्किल है कि ऐसे संविधान को केंद्रीकरण करने वाला कैसे कहा जा सकता है। हो सकता है कि हमारे संविधान में केंद्र को किसी अन्य संघीय संविधान की तुलना में ज्यादा विधायी और कार्यकारी अधिकार दिए गए हों। यह भी हो सकता है कि शेष अधिकार (residuary powers) भी केंद्र को दिए गए हों, न कि राज्यों को। लेकिन ये बातें संघवाद का सार नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, संघवाद की मुख्य पहचान यह है कि विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बँटवारा केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है। यही सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना गलत है कि राज्यों को केंद्र के अधीन कर दिया गया है। केंद्र अपनी इच्छा से इस बँटवारे को बदल नहीं सकता। न्यायपालिका भी ऐसा नहीं कर सकती। जैसा कि ठीक ही कहा गया है:
“न्यायालय संशोधन कर सकते हैं, पूरी तरह पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। वे नई दलीलों और नए दृष्टिकोणों के आधार पर पहले की व्याख्याओं को संशोधित कर सकते हैं, जहाँ केंद्र और राज्य के अधिकारों की सीमाएं मिलती हैं उस रेखा को वे थोड़ा इधर-उधर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएँ हैं जिन्हें वे पार नहीं कर सकते, स्पष्ट रूप से तय किए गए कुछ अधिकारों को वे पुनः विभाजित नहीं कर सकते।”
इस तरह यह पहला आरोप कि संविधान में संघवाद को पराजित करने वाला केंद्रीकरण है गलत साबित होता है।
दूसरा आरोप है कि संविधान में, केंद्र को राज्यों को दरकिनार करने के अधिकार दिए गए हैं। इस आरोप को स्वीकार करना होगा। लेकिन संविधान में ऐसे अधिकार शामिल करने के लिए उसकी निंदा करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये अधिकार संविधान का सामान्य लक्षण नहीं हैं। इनका उपयोग और प्रभाव केवल आपातकाल की स्थितियों तक सीमित है। दूसरी बात यह है कि क्या आपातकाल में केंद्र को ऐसे अधिकार दिए बिना चल सकता है? जो लोग आपातकाल में भी केंद्र को ऐसे अधिकार देने की जरूरत नहीं मानते, उन्हें इस मामले की जड़ में स्थित समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। इस समस्या को प्रसिद्ध “द राउंड टेबल” पत्रिका के दिसंबर 1935 के अंक में एक लेखक ने इतनी स्पष्टता से प्रस्तुत किया है कि मैं इसे उद्धृत करने में कोई संकोच नहीं करता। लेखक कहते हैं :
“राजनीतिक व्यवस्था अधिकारों और कर्तव्यों का एक समूह है जो अंततः इस प्रश्न पर आधारित है कि नागरिक किसके प्रति या किस ऑथोरिटी के प्रति निष्ठा रखता है। सामान्य परिस्थितियों में यह सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि कानून सहज रूप से अपना काम करता है। एक व्यक्ति अपना कामकाज करते हुए एक मामले में एक ऑथोरिटी का पालन करता है और दूसरे मामले में किसी दूसरी ऑथोरिटी का। लेकिन संकट के समय इन दोनों ऑथोरिटीज में टकराव हो सकता है, और ऐसी परिस्थिति में अंतिम निष्ठा में कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। अंतिमतः निष्ठा का सवाल केवल कानूनी व्याख्या से तय नहीं किया जा सकता। कानून को वास्तविकताओं के अनुसार ढलना पड़ता है, वरना कानून ही विफल हो जाता है। जब सारी औपचारिकताएँ ख़त्म हो जाती हैं, तब सवाल उठता है कि नागरिक की अंतिम निष्ठा पर कौनसी सत्ता का हक़ है? केंद्र या राज्य?"
इस समस्या का समाधान इस सवाल के उत्तर पर निर्भर करता है, और यही इस पूरे मुद्दे का सार है। ज्यादातर लोग इससे बिलकुल सहमत होंगे कि आपातकाल में नागरिक की अंतिम निष्ठा केंद्र के प्रति होनी चाहिए, न कि राज्यों के प्रति। क्योंकि सिर्फ केंद्र ही पुरे देश के साझा लक्ष्य और भलाई के लिए काम कर सकता है। यही कारण है कि केंद्र को आपातकाल में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। और आखिरकार, इन आपातकालीन अधिकारों के माध्यम से राज्यों पर क्या दायित्व थोपा गया है? बस इतना ही कि—संकट के समय में, वे अपने स्थानीय हितों के साथ-साथ पूरे राष्ट्र के विचारों और हितों पर भी विचार करें। केवल वही लोग जो इस समस्या को नहीं समझते, इस पर आपत्ति जता सकते हैं।
26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अपनी स्वतंत्रता बरक़रार रख पाएगा या फिर से खो देगा?
मैं यहाँ रुक सकता था लेकिन मेरे मन में अपने देश के भविष्य को लेकर इतने विचार उमड़ रहे हैं कि मुझे लगता है इस अवसर पर मुझे उनमें से कुछ विचारों को व्यक्त करना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह अपनी स्वतंत्रता बरक़रार रख पाएगा या फिर से खो देगा? यह पहला विचार है जो मुझे बेहद बेचैन कर देता है।
ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र नहीं था। भारत स्वतंत्र था लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी। इसलिए मुद्दा यह है कि क्या वह फिर एक बार अपनी स्वतंत्रता खो देगा? यही विचार है जो मुझे भविष्य के बारे में सबसे ज़्यादा चिंतित करता है। जो बात मुझे और भी ज्यादा परेशान करती है, वह यह है कि भारत ने न सिर्फ अपनी आजादी खोई थी, बल्कि वह अपने ही कुछ लोगों की गद्दारी और विश्वासघात के कारण खोई थी।
जब मोहम्मद-बिन-कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब राजा दाहिर के सेनापतियों ने कासिम के गुप्तचरों से रिश्वत ली और अपने ही राजा का साथ नहीं दिया। वह जयचंद ही था जिसने मोहम्मद घोरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज से लड़ने का न्योता दिया, साथ ही उसे युद्ध में अपनी और सोलंकी राजाओं की मदद देने का वादा भी किया। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज़ सिख शासकों को ख़त्म कर रहे थे, तब उनके प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुपचाप बैठे रहे थे और उन्होंने सिख साम्राज्य को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। 1857 में, जब भारत के बड़े हिस्से ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग छेड़ दी थी, तब सिख शासक तमाशबीन बनकर खड़े थे।
क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? यही वह विचार है जो मुझे अत्यधिक चिंतित करता है। यह चिंता और गहरी हो जाती है जब मैं यह सोचता हूं कि जाति और धर्म जैसे हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा अब हमारे सामने अनेक राजनीतिक पार्टियां होंगी, जिनके विचार एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न और विरोधी होंगे। क्या भारतीय नागरिक देश को अपने धर्म और जाति से ऊपर रखेंगे? या फिर अपने धर्म और जाती को देश से ऊपर रखेंगे? मुझे नहीं पता।
लेकिन इतना तो तय है कि अगर पार्टियां अपने संप्रदाय को देश से ऊपर रखेंगी, तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर ख़तरे में पड़ जाएगी...और शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। इस संभावना से हमें हर हाल में बचना होगा। हमें अपने खून के आखिरी कतरे तक अपनी आजादी की रक्षा करनी होगी।
मेरे मन में फिर से वही विचार आता है: क्या भारत अपना यह लोकतांत्रिक संविधान बरक़रार रख पाएगा, या फिर उसे भी खो देगा?
26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा—यानी उस दिन से भारत में जनता की, जनता द्वारा, और जनता के लिए बनी हुई सरकार होगी। मेरे मन में फिर से वही विचार आता है: क्या भारत अपना यह लोकतांत्रिक संविधान बरक़रार रख पाएगा, या फिर उसे भी खो देगा? यह दूसरा विचार है, जो मुझे पहले जितना ही बेचैन करता है।
ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं था। एक समय था जब भारत गणराज्यों से भरा हुआ था। और जहां राजतंत्र था, वह भी या तो निर्वाचित था या सीमित था। कभी भी पूर्णतः निरंकुश नहीं था।
ऐसा नहीं है कि भारत को संसद या संसदीय प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं था। अगर आप बौद्ध भिक्षु संघों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि ये संघ यानी संसद ही थे और संसद के अलावा कुछ नहीं थे। इतना ही नहीं वे आधुनिक समय में ज्ञात सभी संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों को जानते और उनका पालन भी करते थे। उनमें बैठक व्यवस्था, प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, कोरस, व्हिप, मतगणना, मतपत्र द्वारा मतदान, निंदा प्रस्ताव, रेग्युलराईजेशन, Res judicata इत्यादि संबंधी नियम थे। हालाँकि संसदीय प्रक्रिया के इन नियमों को बुद्ध ने संघों की बैठकों के लिए लागू किया था, उन्होंने भी ये नियम उन राजनीतिक सभाओं से ही लिए होंगे, जो उस समय भारत में प्रचलित थीं।
भारत ने यह लोकतांत्रिक व्यवस्था खो दी। क्या वह इसे दुबारा खो देगा? मुझे नहीं पता। लेकिन भारत जैसे देश में—जहां लोकतंत्र इतने लंबे अरसे तक गायब रहा है कि अब उसे एक नई व्यवस्था ही माना जाना चाहिए—लोकतंत्र की जगह तानाशाही आ जाने का पूरा ख़तरा है। ऐसा बिलकुल हो सकता है कि यह नवजात लोकतंत्र अपना बाहरी रूप तो बनाए रखे, लेकिन अंदर से तानाशाही बन जाए। अगर किसी को भारी बहुमत मिलता है, तो यह ख़तरा और बढ़ सकता है।
अगर हम लोकतंत्र को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि वास्तव में भी कायम रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? मेरे विचार से सबसे पहली बात, हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक तरीकों का ही सहारा लेना होगा। इसका मतलब है कि हमें क्रांति जैसे हिंसात्मक तरीकों को त्यागना होगा। हमें सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे तरीकों को भी छोड़ना होगा। जब आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक रास्ते उपलब्ध नहीं थे, तब इन असंवैधानिक तरीकों का महत्व बेशक बहुत ज्यादा था। लेकिन आज जब हमारे पास संवैधानिक रास्ते हैं, तो इन असंवैधानिक तरीकों को अपनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये तरीके ‘अराजकता का व्याकरण’ (Grammar of Anarchy) हैं और कुछ भी नहीं। हम जितना जल्दी इन्हें छोड़ दें, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा।
दूसरी बात जो हमें अवश्य करनी होगी, वह है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लोकतंत्र के चहेतों को दी गई चेतावनी का पालन—अर्थात, "कभी भी अपनी आजादी किसी महान व्यक्ति के चरणों में अर्पित मत करो, और न ही उसे इतने अधिकार दो कि वह तुम्हारी संस्थाओं को ही नष्ट कर सके।" देश की सेवा करने वाले महान लोगों के प्रति कृतज्ञ होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। जैसा कि आयरलैंड के सपूत डैनियल ओ'कॉनेल ने कहा है कि,
“कृतज्ञता के नाम पर किसी भी पुरुष से उसका आत्मसम्मान नहीं छिना जा सकता, कृतज्ञता के नाम पर किसी भी स्त्री से उसकी पवित्रता नहीं छिनी जा सकती, और कृतज्ञता के नाम पर किसी भी राष्ट्र से उसकी आजादी नहीं छिनी जा सकती।”
भारत के लिए यह सावधानी अन्य किसी भी देश से ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे हम श्रद्धा या ‘व्यक्ति-पूजा’ कह सकते हैं, राजनीति में इतनी गहराई तक समाई हुई है जितनी किसी और देश में नहीं है। धर्म में तो भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में यही भक्ति या व्यक्ति-पूजा, निश्चित ही पतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाती है।
तीसरी बात जो हमें करनी होगी वह है केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर संतुष्ट न होना। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र के मूल में अगर सामाजिक लोकतंत्र न हो तो वह टिक नहीं सकता। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को जीवन के सिद्धांत के रुप में स्वीकार किया गया है।
इन तीनों तत्वों को अलग-अलग नहीं देखना चाहिए, बल्कि तीनों को एक साथ एक त्रिपुटी के रूप में देखना चाहिए। अगर आप इसमें से किसी एक को अलग कर दें, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। ना ही बंधुता को स्वतंत्रता और समानता से अलग किया जा सकता है।
समानता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ लोगों का प्रभुत्व प्रस्थापित कर देती है। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल और सोच को मार देती है। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से नहीं टिक सकती। फिर उन्हें लागू करने के लिए आपको बल का प्रयोग करना पड़ता है।
26 जनवरी 1950 को हम एक प्रचंड विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहाँ हमारी राजनीति में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी।
हमें शुरुआत में ही यह स्वीकार करना होगा कि भारत में दो चीजों का पूर्ण अभाव है। जिनमें से एक है समानता। हमारा सामाजिक ढांचा ‘श्रेणीबद्ध असमानता’ (graded inequality) पर आधारित है। यह ऐसा समाज है जिसमें एक ओर कुछ लोगों के पास अपार संपत्ति है, वहीं दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम एक प्रचंड विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहाँ हमारी राजनीति में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। राजनीति में हम ‘एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट, एक मूल्य’ के सिद्धांत को मानेंगे, लेकिन हमारे सामाजिक-आर्थिक ढांचे के कारण, हम ‘एक व्यक्ति, एक मूल्य’ के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक यह विरोधाभासों से भरा जीवन जीते रहेंगे? हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से कब तक मुंह मोड़ते रहेंगे? लंबे समय तक इसे नकारना हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा होगा। हमें जितनी जल्दी हो सके इस विरोधाभास को खत्म करना होगा। वरना असमानता से पीड़ित लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ही नष्ट कर देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है।
हमारे समाज में जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है, वह है ‘बंधुता’। बंधुता का मतलब क्या है? बंधुता या बंधूभाव का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच एक समान भाईचारे की भावना, यह भावना कि हम सभी भारतीय एक हैं। यह वह तत्व है जो सामाजिक जीवन में एकता और एकात्मता लाता है। यह भावना पैदा करना आसान नहीं है। यह कितना मुश्किल काम है इसका अंदाजा उस घटना से लगाया जा सकता है, जिसका उल्लेख जेम्स ब्राइस ने अपनी किताब American Commonwealth में अमेरिका के बारे में किया है।
यह घटना—जिसे मैं ब्राइस के ही शब्दों में दोहराना चाहूँगा — इस प्रकार है :
"कुछ साल पहले, अमेरिकी प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च अपनी त्रैवार्षिक सभा में अपनी प्रार्थना-पद्धति (liturgy) में संशोधन कर रहा था। यह सोचकर कि छोटी प्रार्थनाओं में पूरे देश के लिए भी एक प्रार्थना शामिल करना अच्छा होगा, न्यू इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित धार्मिक विद्वान ने ये शब्द प्रस्तावित किए — 'हे प्रभु, हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दें। दोपहर को बिना ज्यादा विचार किए यह वाक्य स्वीकार कर लिया गया, लेकिन दूसरे दिन इसपर पुनर्विचार करना पड़ा। आम नागरिकों की ओर से 'राष्ट्र' शब्द को लेकर इतनी आपत्तियाँ उठाई गईं—क्योंकि यह शब्द राष्ट्रीय एकता को बहुत स्पष्ट रूप से मान्यता देता था—इसे हटाना पड़ा और इसकी जगह यह वाक्य अपनाया गया: 'हे प्रभु, इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दें।'”
यह घटना जब हुई उस समय अमेरिका में इतनी कम एकजुटता थी कि वहाँ के लोग खुद को एक राष्ट्र तक नहीं मानते थे। अगर अमेरिका के लोग अपने को राष्ट्र मानने में झिझकते थे, तो यह समझना आसान है कि भारत के लोगों के लिए अपने आपको राष्ट्र मानना कितना कठिन रहा होगा।
मुझे वे दिन याद हैं जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय “भारत के लोग” इन शब्दों से घृणा करते थे। उन्हें “भारतीय राष्ट्र” कहना ज्यादा पसंद था। लेकिन मेरी राय में, यह मान लेना कि हम पहले से ही एक राष्ट्र हैं, एक बहुत बड़ा भ्रम है। हजारों जातियों में बंटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि हम सामाजिक और मानसिक रूप से अभी तक एक राष्ट्र नहीं बने हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि तभी हम राष्ट्र बनने की आवश्यकता को समझ पाएंगे और इसे साकार करने के उपायों पर गंभीरता से विचार कर सकेंगे। लेकिन यह लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन होगा—अमेरिका से भी बहुत कठिन, क्योंकि अमेरिका में जाती की कोई समस्या नहीं है, भारत में जातियां हैं।
जाती राष्ट्र-विरोधी है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि वह सामाजिक जीवन में विभाजन पैदा करती है। दूसरा, यह जातियों के बीच ईर्ष्या और वैरभाव उत्पन्न करती है। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों पर विजय पानी होगी। क्योंकि बंधुता तब ही पैदा हो पाएगी जब हम एक राष्ट्र बनें। अगर बंधुता नहीं होगी, तो समानता और स्वतंत्रता ऊपरी लीपा-पोती की तरह सिर्फ दिखावे की चीजें बनकर रह जाएंगी।
ये मेरे विचार हैं उन कामों के बारे में जो हमारे सामने हैं। शायद ये कुछ लोगों को अप्रिय लगें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस देश में राजनीतिक सत्ता एक लंबे समय तक कुछ लोगों का एकाधिकार (monopoly) रही है। बाकी लोग सिर्फ बोझ ढोने वाले जानवरों जैसे ही नहीं, बल्कि शिकार बनने वाले जानवरों जैसे भी रहे हैं। इस एकाधिकार ने न सिर्फ उन्हें बेहतर जीवन के अवसरों से वंचित किया है, बल्कि उनके जीवन का महत्व ही नष्ट कर दिया है। ये शोषित वर्ग 'शासित' होने से थक चुके हैं। अब वे खुद पर शासन करने के लिए अधीर हैं। शोषितों की इस आत्म-जागृती की तीव्र आकांक्षा को हमें वर्ग-संघर्ष या वर्ग-युद्ध (class-war) में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सदन में विभाजन हो जाएगा जाएगा और वह सच में एक बड़ी आपदा होगी। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, "भीतर से बंटा हुआ घर ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता।"
इसलिए, जीतनी जल्दी इन वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, उतना ही बेहतर होगा उन कुछ लोगों के लिए, देश के लिए, इसकी आजादी कायम रखने के लिए और इसके लोकतांत्रिक ढांचे को बरक़रार रखने के लिए भी। यह सब तभी संभव है जब हम जीवन के हर क्षेत्र में समानता और बंधुता की स्थापना कर पाएँगे। इसीलिए मैंने इन दोनों मूल्यों पर इतना ज़ोर दिया है।
आजादी निस्संदेह खुशी की बात है। लेकिन हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि इस आजादी ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाल दी हैं।
मैं अब सदन को और अधिक थकाना नहीं चाहता। आजादी निस्संदेह खुशी की बात है। लेकिन हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि इस आजादी ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी डाल दी हैं। अब हमारे पास ब्रिटिश शासन को दोष देने का बहाना नहीं बचा है। अब अगर कुछ गलत होता है, तो दोषी सिर्फ और सिर्फ हम ही होंगे। और चीजें गलत दिशा में जाने का पूरा खतरा है। वक्त तेजी से बदल रहा है। हमारे अपने लोगों सहित सभी नई विचारधाराओं से प्रभावित हो रहे हैं। वे अब 'जनता द्वारा' बनी सरकार से ऊब चुके हैं। अब वे केवल 'जनता के लिए सरकार' चाहते हैं, फिर भले ही वह सरकार 'जनता की' और 'जनता द्वारा' न भी हो।
अगर हम उस संविधान को बचाना चाहते हैं जिसमें हमने 'जनता की, जनता के लिए, और जनता द्वारा सरकार' के सिद्धांत को स्थापित किया है, तो हमें हमारे रास्ते में खड़ी बुराइयों को पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए, और न ही उन्हें दूर करने की अपनी कोशिशों में कमी रखनी चाहिए। यही देश सेवा का एकमात्र तरीका है। मुझे इससे बेहतर कोई तरीका नहीं पता।
बाबासाहब का मूल अंग्रेजी भाषण यहाँ पढ़ सकते हैं: https://www.constitutionofindia.net/debates/25-nov-1949/
We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर हमने अपनी पुलियाबाजी कई एपिसोड किए हैं, उन्हें भी जरूर सुनिए और शेअर कीजिए!
अम्बेडकर के जातिप्रथा पर विचार: भाग १. Ambedkar on Caste Part 1
गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम भीमराव अम्बेडकर के योगदान को अक़्सर सलामी देते हैं | पर अम्बेडकर साहब जैसे बुद्धिजीवी को सम्मान देने का शायद सबसे प्रभावशाली तरीका है उनके विचारों को समझना| अब उनको पुलियाबाज़ी में ला पाना तो संभव नहीं है इसलिए इस बार हमने प्रयत्न किया उनके कुछ लेख पढ़ने का और उनके तर्क को आपके सामने रखने का | इस दो भाग स्पेशल में हमने विश्लेषण क…
अम्बेडकर के जातिप्रथा पर विचार : भाग २. Ambedkar on Caste Part 2
पूरे भारत ने अपना सत्तरवाँ गणतंत्र दिवस पिछले हफ़्ते मनाया और अंबेडकर के योगदान को फिर एक बार याद किया | पर अंबेडकर साहब जैसे बुद्धिजीवी को सम्मान देने का शायद सबसे प्रभावशाली तरीका है उनके विचारों को समझना | अब उनको पुलियाबाज़ी में ला पाना तो संभव नहीं है इसलिए इस बार हमने प्रयत्न किया उनके कुछ लेख पढ़ने का और उनके तर्क को आपके सामने रखने का | इस दो भाग स…
अंबेडकर की विचार यात्रा। The Life and Ideas of Dr. BR Ambedkar ft. Ashok Gopal
पुलियाबाज़ी पर हर साल गणतंत्र दिवस पर हम संविधान या उससे जुड़े विषयों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इस साल हमने सोचा कि क्यों न हमारे संविधान के प्रमुख रचयिता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों को और गहराई से समझा जाये। इस विषय पर पुलियाबाज़ी के लिए हमारे मेहमान है अशोक गोपाल जी जिन्होंने २० वर्षों की रिसर्च के बाद डॉ.अंबेडकर की जीवनी लिखी है। चर्चा के दौ…
अंबेडकर का घोषणा पत्र। Ambedkar’s Manifesto for India.
In this Constitution Day Special episode, we discuss Dr. Ambedkar’s ideas through the only election manifesto he ever wrote. Listen in.
दलित पूंजीवाद. Dalit Capitalism.
Well-known journalist, author, and entrepreneur Chandran Bhan Prasad (@cbhanp) is on Puliyabaazi to discuss his latest book What is Ambedkarism?. Mr Prasad makes a case for capitalism as a way for achieving Dalit empowerment. In this episode, we also discuss Ambedkar’s ideas on dalit politics and economics.