The Use of Knowledge in Society: समाज में संसाधनों का वितरण कैसे हो?
अर्थशास्त्र के सार्वकालिक महान विचारों में से एक ‘द यूज़ ऑफ़ नॉलेज..' का सारांश
Dear Reader,
We are thrilled to introduce you to our newest team member, Parikshit, who joins us as an editor. In the coming days, you will read more of his articles and translations on our Substack. He will also provide editorial support for submissions from our readers.
Parikshit brings over a decade of experience as a writer-translator in the environment, social, and education sectors. His articles and translations have been published in prominent national and regional newspapers and magazines. He has also co-authored and translated several children's books. In today’s Tippani, Parikshit shares a concise summary of the classic essay ‘The Use of Knowledge in Society’ by Friedrich A. Hayek in simple Hindi. This is part of our series to ensure that great ideas are made accessible to Hindi readers as well.
तो पढ़िए और बताइये कि लेख कैसा लगा? लेख पसंद आये तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें।
सन 1945 में ऑस्ट्रियाई-ब्रिटिश अर्थशास्त्री फ़्रेडरिक हायेक ने ‘द यूज़ ऑफ़ नॉलेज इन सोसाइटी’ (समाज में ज्ञान का उपयोग) शीर्षक से एक लेख लिखा। उस समय की प्रसिद्ध आर्थिक पत्रिका अमेरिकन इकोनोमिक रिव्यू में प्रकाशित इस लेख की ना सिर्फ़ उस वक्त काफी चर्चा हुई बल्कि आज भी इसे आधुनिक अर्थशास्त्र को दिशा देने वाले चुनिंदा दस्तावेजों में से एक माना जाता है। इस लेख में हायेक ने केंद्रीकृत (Centralised) निर्णय-प्रक्रिया की मर्यादाएं दर्शाते हुए, विकेंद्रित (Decentralised) निर्णय-प्रक्रिया की अहमियत को विस्तार से समझाया है। आइए, ‘द यूज़ ऑफ़ नॉलेज इन सोसाइटी’ को कुछ समकालीन उदाहरणों के साथ सारांश रूप से समझने की कोशिश करते हैं।
विकेंद्रित ज्ञान
फ़्रेडरिक हायेक अपने लेख की शुरुआत ही अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण सवाल से करते हैं – समाज संसाधनों के वितरण के लिए अपने ज्ञान का प्रभावी रूप से उपयोग कैसे कर सकता है? यहाँ पर ज्ञान से हायेक का तात्पर्य बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों, सेवाओं आदि से संबंधित ज्ञान से है। वास्तविकता यह है कि यह ज्ञान किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होता बल्कि यह लाखों व्यक्तियों में फैला हुआ होता है, जो अपनी परिस्थिति, प्राथमिकता, और अवसर के आधार पर निर्णय लेते हैं।
उदाहरण के लिए किसी गाँव में रहने वाला एक व्यक्ति क्या चाहता है—दाल, गेहूं, मोबाइल या मोटरसाइकिल—ये तो वही बता सकता है। इनमें से कौन सी चीज पर कितना खर्च करना है, इसका निर्णय भी वही ज्यादा अच्छी तरह से ले सकता है। उसी गाँव का दुकानदार अपने गाँव के ग्राहक क्या खरीदते हैं, यह बेहतर जानता है। गाँववाले और दुकानदार दोनों ही अपनी पसंद और परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेते हैं। यदि सरकार को इन दोनों की ओर से निर्णय लेना हो तो उसे इन दोनों की पसंद-नापसंद, आर्थिक क्षमता आदि की जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। जब यह बात दो लोगों तक सीमित हो तब शायद यह संभव लग सकता है, लेकिन जब यही निर्णय देश के सभी शहरों और गांवों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना हो तो, क्या यह संभव हो पाएगा?
सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की विफलता
हायेक कहते हैं कि सवाल यह नहीं है कि प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि प्लानिंग कैसे होनी चाहिए – किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या कई विकेंद्रित व्यक्तियों द्वारा। अगर हमें केंद्रीय प्लानिंग सफल करनी है तो हमें, सभी उत्पादों, सेवाओं, सप्लाई चेन आदि से संबंधित सारी जानकारी एक जगह पर इकट्ठा करनी होगी। इस जानकारी में जितनी कमी रहेगी प्लानिंग उतनी ही कमजोर होगी। दूसरी बात, हमें यह जानकारी निरंतर अपडेट भी करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों की परिस्थिति, भावनाएं, और विचार निरंतर बदलते रहते हैं और उसी तरह उनके निर्णय भी।
लोगों के पास जो व्यक्तिगत ज्ञान होता है उसका उपयोग वे अपनी रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में करते हैं। यह स्थानीय ज्ञान न होने से, योजनाकार ऐसे निर्णय लेते हैं जो संसाधनों की कमी, surplus या बर्बादी का कारण बनते हैं। जैसे किसानों को अपनी जमीन, पानी, स्थानीय मौसम और बाजार का ज्ञान होता है और उनके आधार पर वे अपनी फसल का निर्णय लेते हैं। यदि सरकार देश के सभी किसानों को एक ही तरह से खेती करने पर मजबूर करे तो क्या होगा? श्रीलंका में विफल साबित हुआ जैविक खेती प्रयोग और उसके भयावह परिणाम इसका जीता-जागता उदाहरण है।
कल्पना कीजिए, आप किसी शॉपिंग मॉल में किराना माल लेने गए और वहाँ आपको कुछ और वस्तुएं दिखीं। इस वक्त आपको लगा कि इनमें से कुछ आपको खरीदनी चाहिए। अब क्या आप उन्हें खरीदेंगे? इसके लिए अपना किराना माल कम करेंगे? या नहीं खरीदेंगे? ये सभी निर्णय आपके उस वक्त के विचार, भावनाएं आदि पर निर्भर करते हैं। अब आप जैसे लाखों, करोड़ों लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं, उन सभी के विचारों को उसी क्षण किसी एक जगह पर रिकॉर्ड करना कैसे संभव हो सकता है?
अब कोई कह सकता है कि आजकल तो सुपर कंप्यूटर आ चुके हैं जिनमें दुनियाभर का डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात की ओर ध्यान देना जरूरी है: व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला ‘डेटा’ सिर्फ व्यक्तियों की उस वक्त की परिस्थिति ही नहीं होती, उनके विचार और भावनाएं भी होते हैं, जो की बेहद निजी और निरंतर बदलने वाले होते हैं। इतने सारे व्यक्तियों के इतने सारे ‘डेटा’ पर तत्क्षण प्रक्रिया कर सके ऐसा सुपर कंप्यूटर तो आज तक बना नहीं है।
Price as a Signal: विकेंद्रित संचार माध्यम
हायेक कहते हैं कि क़ीमत एक जादुई चीज़ है—वस्तुओं की कीमतें सिर्फ़ एक नंबर नहीं है बल्कि वे एक विकेंद्रित संचार माध्यम (Decentralised Signal) का काम करती हैं। किसी वस्तु की कीमत और आपूर्ति के आधार पर लोग अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, यहाँ उन्हें किसी केंद्रीय मदद की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुओं की कीमतों में निरंतर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और इन उतार-चढ़ाव के कारणों को जाने बगैर भी लोग अपने निर्णय बदल लेते हैं।
यहाँ हायेक टिन धातु का उदाहरण देते हैं जो आज भी लागू होता है। अगर किसी खान (माइन) के बंद होने से या टिन का कोई बेहतर वैकल्पिक उपयोग विकसित होने से, टिन की आपूर्ति घट जाती है, तो टिन की कीमतें बढ़ जाएंगी। ऐसा होते ही, बिना किसी सरकारी आदेश के, निर्माता टिन का उपयोग कम करने लगेंगे। उपभोक्ता टिन से बने उत्पादों की अपनी मांग को स्वतः कम कर देंगे। यह सब कुछ हो जाएगा बिना इस जानकारी के कि टिन की कमी क्यों हुई। ज़रूरत है सिर्फ़ क़ीमतों के संचार की।

दूसरी ओर टिन की कमी होने से निर्माता उसके विकल्प तलाशेंगे। जहाँ-जहाँ टिन का इस्तेमाल होता है, वहाँ की जरूरतों के अनुसार विकल्प विकसित किए जाएँगे। और उन विकल्पों की अपनी एक नई सल्पाई चेन विकसित होगी। टिन की तरह ही बाजार की अन्य वस्तुओं की मांग-आपूर्ति भी इसी तरह पूरी होगी। यहाँ पर किसी को भी बाजार की पूरी जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं होगी। सभी को अपने लिए जीतनी जानकारी आवश्यक है उतनी मिलते ही वे अपने निर्णय लेंगे।

यही सेल्फ-रेग्युलेशन (स्वयं-नियमन) बाजारों को कारगर बनाता है। कीमतें केवल Supply और Demand को ही नहीं दर्शातीं, वे यह भी दर्शाती हैं कि लाखों लोग किस प्रकार एक-दूसरे को न जानते, पहचानते और बात करते हुए भी सुसंगत निर्णय ले सकते हैं।
ज्ञान की समस्या
हायेक का मानना है कि, समाज में दो प्रकार का ज्ञान होता है।
वैज्ञानिक ज्ञान (Scientific Knowledge) – इसका स्वरूप वैश्विक होता है। यह हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के लिए समान होता है, जैसे भौतिकशास्त्र या गणित के सिद्धांत।
अनुभवजन्य ज्ञान (Tacit Knowledge) – इसे हम बाजार का व्यावहारिक ज्ञान कह सकते, जो अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है । यह ज्ञान व्यक्ति को कोई ‘देता’ नहीं है, यह तो उसे अपने काम और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसे कौशल या हुनर भी कहा जा सकता है। बाजार में विभिन्न व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, जिसके उपयोग से वे अपनी जीविका कमाते हैं। यह सारा ज्ञान इतना व्यापक होता है कि, इसे केंद्रीकृत करना संभव नहीं।
उदाहरण के तौर पर, एक कुशल कारीगर अपने अनुभव से जानता है कि, किसी उत्पाद को कुशलतापूर्वक कैसे बनाया जाए। वहीं एक उद्यमी जानता है कि, उस कारीगर की कुशलता का उपयोग कर के बनाए गए उत्पादन कहाँ और कैसे बेचे जाएँ। इस प्रकार का ज्ञान रिपोर्ट या डेटाबेस में पूरी तरह से कैद नहीं किया जा सकता।
लेकिन केंद्रीय योजनाकार अक्सर सैद्धांतिक, जनरलाज्ड ज्ञान पर अधिक निर्भर रहते हैं और अनुभवजन्य ज्ञान की अनदेखी कर देते हैं। इससे ऐसी नीतियाँ बनती हैं, जो सिद्धांत में तो तार्किक लगती हैं, लेकिन व्यवहार में असफल हो जाती हैं क्योंकि वे उन स्थानीय विवरणों की अनदेखी करती हैं, जिन्हें केवल वहाँ रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं।
स्वयं-निर्मित व्यवस्था
हायेक कहते हैं कि, जब व्यक्ति अपने स्वयं के ज्ञान और प्रोत्साहनों (इंसेंटिव) के आधार पर काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्था उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था किसी मशीन की तरह नहीं है जिसे एक केंद्रीय संचालक की आवश्यकता हो, यह तो एक इकोसिस्टम की तरह है जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से बातचीत करते हैं और समन्वय और सहयोग के पैटर्न विकसित करते हैं।
उदाहरण के लिए, बाजार में कौन क्या बेचे और किस कीमत पर बेचे, यह निर्धारित करने के लिए किसी केंद्रीय अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती। विक्रेता स्पर्धा करते हैं, खरीदार अपने चुनाव करते हैं, और समय के साथ एक प्रभावी प्रणाली विकसित होती है। किसी व्यक्ति को पूरी प्रणाली के बारे में संपूर्ण ज्ञान न होते हुए भी यह प्राकृतिक समन्वय हो जाता है।
हायेक के विचार यह समझने में मदद करते हैं कि मुक्त बाजार (Free Market) आमतौर पर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक कारगर क्यों होता है। कुछ ऐतिहासिक उदाहरण उनके तर्क को और मजबूत करते हैं:
सोवियत संघ को उत्पादन, मांग और आपूर्ति से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे अप्रभावी उत्पादन (Inefficient Production) और लगातार कमी (Chronic Shortages), क्योंकि सरकार ने हर चीज का प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर करने की कोशिश की। कीमतों के संकेतों (Price Signals) और स्थानीय अनुकूलन (Local Adaptation) के अभाव में, यह प्रणाली लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने बाजार-आधारित सुधारों (Market-Based Reforms) को अपनाकर तेजी से आर्थिक पुनर्निर्माण किया। विकेंद्रित निर्णय-प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था को तेजी से पुनर्जीवित करने में मदद की।
इस प्रकार हायेक का मूल संदेश था, समाज में ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग केंद्रीय नियंत्रण के माध्यम से नहीं बल्कि विकेंद्रित निर्णय-प्रक्रिया से किया जा सकता है। क़ीमते इस विकेंद्रित निर्णय-प्रक्रिया का माध्यम है और इसीलिए सरकार का क़ीमत से छेड़छाड़ करना बहुत हानिकारक होता है। आर्थिक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होती, इससे संपूर्ण समाज को सभी व्यक्तियों के ज्ञान का लाभ मिलता है। सबसे अच्छी आर्थिक प्रणालियाँ वही हैं जो व्यक्तिगत ज्ञान और प्रेरणाओं का सम्मान और उपयोग करती हैं।
हायेक के सिद्धांतों को समझकर, हम ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं जो अधिक रिस्पोंसिव हो, कार्यक्षम हो और बदलती दुनिया के अनुरूप हो।
—परीक्षित सूर्यवंशी
फ़्रेडरिक हायेक का मूल लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: https://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw.html



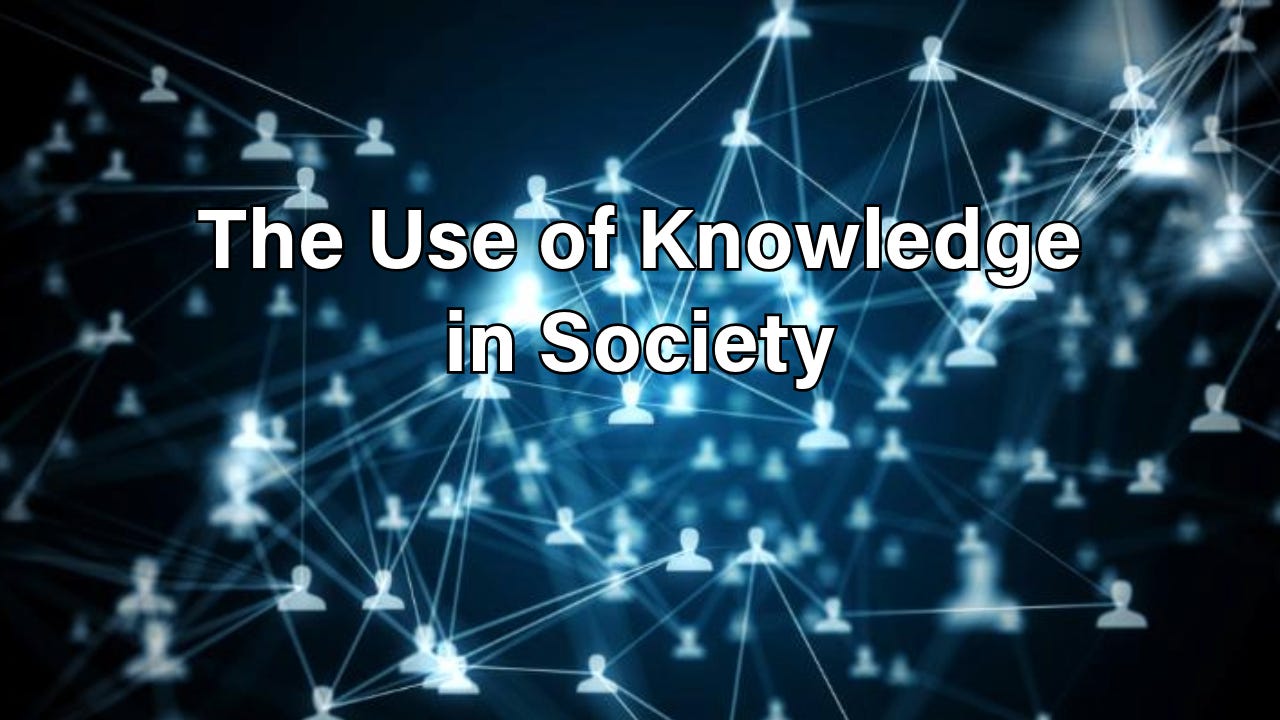
Thank you for the article. I'm trying to better my hindi by reading it. Also, I think these two sentences need a look see if I'm not wrong. If I am wrong, please feel free to let me know.
1. ऐसा होते ही, बिना किसी सरकारी आदेश के, निर्माता टिन का उपयोग कम करने लगेंगे।
2. दूसरी ओर टिन की कमी होने से निर्माता उसके विकल्प तलाशेंगे